मिर्ज़ा ग़ालिब जीवन परिचय ग़ालिब का असल नाम मिर्ज़ा असद उल्ला बैग खान था | आपका जन्म 27 दिसम्बर, 1796 ई. को अकबराबाद में हुआ जो कि अब आगरा के नाम से जाना
मिर्ज़ा ग़ालिब जीवन परिचय
मिर्ज़ा ग़ालिब का असल नाम मिर्ज़ा असद उल्ला बैग खान था | आपका जन्म 27 दिसम्बर, 1796 ई. को अकबराबाद में हुआ जो कि अब आगरा के नाम से जाना जाता है | उनके दादा कौकान बेग खां, शाह आलम के अहद ( शासन काल) में समरकंद से आगरा ( अकबराबाद) आए थे ग़ालिब के परदादा तर्संमखा समरकंद में रहते थे और सैनिक सेवा में थे आपके पुत्र कौकान बेग अपने पिता से लड़कर हिन्दुस्तान चले आए थे उनकी भाषा तुर्की थी | आपके चार बेटे और तीन बेतिया थी | बेटो में अब्दुल्ला बेग और नसरुल्लाबेग का वर्णन मिलता है | यही अब्दुल्ला बेग ग़ालिब के पिता थे | मिर्ज़ा की एक बड़ी बहन खानम, और भाई मिर्ज़ा युसूफ थे | मिर्ज़ा ग़ालिब के पिता फौजी नौकरी में थे इस कारण आपका लालन-पालन ननिहाल में ही हुआ | जब ग़ालिब पांच साल के थे तभी आपके पिताजी का देहावसान हो गया |
हां रंग लायेंगी हमारी फाकामस्ती इक दिन
कहते है की ग़ालिब का है अंदाजे बयाँ और

गुलज़ार साहब मिर्ज़ा ग़ालिब के लिए कहते है
सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के क़सीदे
गुङगुङाते हुई पान की वो दाद-वो, वाह-वा
दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा-से कुछ टाट के परदे
एक बकरी के मिमयाने की आवाज़ !
और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अँधेरे
ऐसे दीवारों से मुँह जोड़ के चलते हैं यहाँ
चूड़ीवालान के कटड़े की बड़ी बी जैसे
अपनी बुझती हुई आँखों से दरवाज़े टटोले
इसी बेनूर अँधेरी-सी गली क़ासिम से
एक तरतीब चिराग़ों की शुरू होती है
एक क़ुरआने सुख़न का सफ़्हाखुलता है
असद उल्लाह ख़ाँ 'ग़ालिब' का पता मिलता है - गुलज़ार
ग़ालिब के चचा जान की भी जल्द ही मृत्यु हो जाने पर वो ननिहाल आ गए. उनका बचपन ननिहाल ही में बीता और बड़े मज़े से बीता | उन लोगों के पास काफी जायदाद थी. ग़ालिब के चचा जान की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो पाँच हज़ार रुपये सालाना पेंशन मिलती थी उसमें 750-750 रुपए ग़ालिब और ग़ालिब के भाई मिर्ज़ा युसूफ का हिस्सा आता था |
ग़ालिब की ननिहाल में मज़े से गुजरती थी, आराम ही आराम था | एक ओर खुशहाल परन्तु पतनशील उच्च मध्यमवर्ग की जीवन-विधि के अनुसार उन्हें पतंग शतरंज और जुए की आदत लगी, दूसरी ओर उच्चकोटि के बुजुर्गों की सोहबत का लाभ मिला |
मिर्ज़ा ग़ालिब ने फ़ारसी की प्रारंभिक शिक्षा आगरा के उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान मौलवी मोहम्मद मोवज्ज़म से प्राप्त की | 1810-1811 ई. में मुल्ला अब्दुस्समद जोईरान के प्रतिष्ठित एवं वैभवसंपन्न व्यक्ति थे, ईरान से घूमते हुए आगरा आये और इन्हें के यहाँ दो साल रहे | इन्हीं से दो साल तक मिर्ज़ा ग़ालिब ने फारसी तथा अन्य काव्य की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया | अब्दुस्समद इनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी सारी विद्या इनमें उड़ेल दी | उच्च प्रेरणाएं जगाने का काम शिक्षण से भी ज्यादा उस वातावरण ने किया जो उनके इर्द-गिर्द था | जिस मोहल्ले में वह रहते थे, वह(गुलाबखाना) उस ज़माने में फारसी भाषा के शिक्षण का एक उच्च केंद्र था | उनके इर्द गिर्द एक से बढ़कर एक फारसी के विद्वान रहते थे|
तस्वीर का दूसरा रूख़ यह भी था कि दुलारे थे, रुपये पैसे की कमी ना थी, किशोरावस्था, <तबियत में उमंगें, यार-दोस्तों के मजमे, खाने-पीने, शतरंज, पतंगबाज़ी, यौवनोंमाद-सबका जमघट | इनकी आदतें बिगड़ गयीं | हुस्न के अफ़सानों में मन उलझा, चन्द्रमुखियों ने दिल को खींचा | 24-25 बरस तक खूब रंगरेलियां कीं पर बाद में उच्च प्रेरणाओं ने इन्हें ऊपर उठने को बाध्य किया | बचपन से ही इन्हें शेरो-शायरी की लत थी | इश्क़ ने उसे उभारा- गो वह इश्क़ बहुत छिछला और बाजारू था |
पच्चीस साल की उम्र में दो हज़ार शेरों का दीवान तैयार हो गया था | इसमें वही चूमा-चाटी,वही स्त्रैण भावनाएँ वही पिटे पिटाये मज़मून थे| जिसमें बाद में अच्छी समझ पैदा होने उसमें कांट छाँट की और अच्छे शेरों को और दुरुस्त किया | एक बार उनके किसी हितैषी ने इनके कुछ शेर मीर तक़ी मीर को सुनाये | सुनकर मीर ने कहा अगर इस लड़के को कोई कामिल (योग्य) उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा वरना महमिल (निरर्थक) बकने लगेगा" मीर की मृत्यु के समय ग़ालिब केवल तेरह वर्ष के थे और दो ही तीन साल पहले उन्होंने शेर कहने शुरू किये थे |
शुरू में ही इस किशोर कवि की ग़ज़ल इतनी दूर लखनऊ में खुदाए-सखुन मीर के सामने पढ़ी गयी और मीर ने जो बड़ों बड़ों को ख़ातिर में नहीं लाते थे इनकी सुप्त प्रतिभा को देखकर इनकी रचनाओं पर सम्मति दी इससे जान पड़ता है कि प्रारम्भ से ही इनमें उच्च कवि के बीज थे |
जब यह सिर्फ तेरह वर्ष के थे, इनका निकाह लोहारू के नवाब अहमदबख्शखाँ के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्शखाँ मारुफ़ की लड़की उमराव बेगम के साथ 9 अगस्त, 1810ई. को संपन्न हुआ था | उस वक़्त उमराव बेगम ग्यारह साल की थीं | विवाह के कुछ वर्ष बाद आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गयी और बाद के साल उन्होंने थोड़ी कठिनाई से बिताये | आर्थिक तंगी चलती ही रहती थी | आय के स्त्रोत कम थे और उनके खर्चे ज्यादा |
मिर्ज़ा ग़ालिब अपने विवाह के कुछ दिनों बाद से ही अपनी ससुराल दिल्ली चले आये और दिल्ली के ही हो गये | उनके ससुर ने उन्हें घर जमाई के रूप में दिल्ली में ही बुला लिया तब से वे वही बस गए | उनके अब्बा का जन्म आगरा में ही हुआ था | उनका विवाह भी कई मुश्किलों के दौर से गुजरा उनके यहाँ सात बच्चो का जन्म हुआ मगर कोई जिन्दा न रह सके |
उनका पूरा नाम "असद-उल्ला खां उर्फ़ 'मिर्ज़ा नौशा' था | वे पहले 'असद' तखल्लुस से लिखते थे पर यह किसी और के उपयोग में आने के कारण उन्होंने अपना तखल्लुस "ग़ालिब" रख लिया और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए | उनका मिजाज बहुत अलग हुआ करता था वे क़र्ज़ लेने से नहीं कतराते थे मगर किसी से मदद लें ऐसा सो कदापि संभव नहीं था तभी तो उन्होंने कहा है -
क़र्ज़ की पीते थे लेकिन समझते थे कि
और खुद के बारे में वो कहते थे
है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे
ग़ालिब का यूँ तो असल वतन आगरा था लेकिन किशोरावस्था में ही वे दिल्ली आ गये थे । कुछ दिन वे ससुराल में रहे फिर अलग रहने लगे । चाहे ससुराल में या अलग उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा दिल्ली की गली क़ासिमजान में बीता । सच पूंछें तो इस गली के चप्पे-चप्पे से उनका अधिकांश जीवन जुड़ा हुआ था । वे पचास-पचपन वर्ष दिल्ली में रहें जिसका अधिकांश भाग इसी गली में बीता । यह गली चाँदनी चौक से मुड़कर बल्लीमारान के अन्दर जाने पर शम्शी दवाख़ाना और हकीम शरीफ़खाँ की मस्जिद के बीच पड़ती है । इसी गली में ग़ालिब के चाचा का ब्याह क़ासिमजान (जिनके नाम पर यह गली है ।) के भाई आरिफ़जान की बेटी से हुआ था और बाद में ग़ालिब ख़ुद दूल्हा बने आरिफ़जान की पोती और लोहारू के नवाब की भतीजी उमराव बेगम को ब्याहने इसी गली में आये । साठ साल बाद जब बूढ़े शायर का जनाज़ा निकला तो इसी गली से गुज़रा । और अंततः वे इस दुनिया-ए-फानी से 15 फरवरी, 1869 को रुखसत हो लिए |
उनके बारे में गुलजार साहब लिखते है :-
बल्ली मारां की वो पेचीदा दलीलों की-सी गलियाँ
वे बहादूर शाह जफ़र के यहाँ राजकवि के रूप में पदस्थ थे | उनके बारे में कई किस्से मशहूर है उनमे से कुछ पेश है, एक बार शेख इब्राहीम जौक के मुह से यह शेर सुनकर वे उछल पड़े
अब तो घबरा के ये कहते है कि मर जायेंगे !
मर के भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे ?
और इस शेर को सुनकर तो उन्होंने अपने दिवान को देने की पेशकश कर दी
तुम मेरे पास होते हो गोया !
जब कोई दूसरा नहीं होता !!
खैर अब आगे बढ़ते है
एक बार की बात है जब ग़दर के बाद उनकी पेंशन बंद हो गई थी और दरबार में जाने का दरवाजा भी बंद था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब के मीर मुंशी मोतीलाल एक बार फिर मिलने आए | मिर्जा ने उनसे कहा, 'तमाम उम्र में एक दिन शराब न पी हो, तो काफ़िर, और एक दफा नमाज पढ़ी हो, तो गुनाहगार ' फिर मै नहीं जानता कि सरकार ने किस तरह मुझे बागी करार दिया |
वैसे भी उनकी अल्लाह से पटती कहा थी वे तो शायद कभी नमाज भी नहीं पढ़ते थे | इसी से संबध एक किस्सा है ग़दर के दिनों में ही अंग्रेज सभी मुसलमानों को शक की निगाह से देखते थे | दिल्ली मुसलमानों से ख़ाली हो गई थी, पर ग़ालिब और कुछ दुसरे लोग चुपचाप अपने घरो में पढ़े रहे | एक दिन कुछ गोरे इन्हें भी पकड़कर कर्नल ब्राउन के पास ले गए | उस वक़्त 'कुलाह' (उची टोपी) इनके सर पर थी, अजीब वेशभूषा थी | कर्नल ने मिर्ज़ा की यह धज देखी, तो पूछा ' वेल टुम मुसलमान' (Well Tum Musalmaan )' मिर्ज़ा ने कहा- 'आधा' ! कर्नल ने पूछा, ' इसका क्या मटलब है ' तो इस पर मिर्ज़ा बोले,'शराब पीता हू, सूअर नहीं खाता |' कर्नल सुनकर हसने लगा और इन्हें घर जाने की इजाजत दे दी |
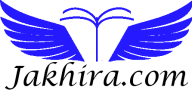




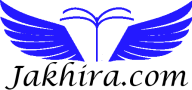





COMMENTS