हिन्दी गज़ल और कृष्ण बिहारी नूर हिन्दी ग़ज़ल के विकास में वही ग़ज़लकार सही अर्थों में सहयोग दे सकते हैं, जो ग़ज़ल के शिल्प और उसकी कोमलता से परिचित हैं। .
हिन्दी गज़ल और कृष्ण बिहारी नूर
हिन्दी ग़ज़ल के विकास में वही ग़ज़लकार सही अर्थों में सहयोग दे सकते हैं, जो ग़ज़ल के शिल्प और उसकी कोमलता से परिचित हैं। इस कार्य को बख़ूबी अंजाम दिया श्री कृष्णबिहारी 'नूर' ने। नूर साहब चूँकि मूलरूप से ग़ज़लकार थे और उर्दू से उन्होंने हिन्दी में पदार्पण किया, इसलिए वे ग़ज़ल के शिल्पविधान और उसकी बारीकियों से भलीभाँति परिचित थे। यही कारण है कि उनकी ग़ज़लें जहाँ शिल्प की दृष्टि से मज़बूत हैं, वहीं कथ्य की दृष्टि से परिपक्व। नूर साहब चूँकि मुशायरों और कवि-सम्मेलनों से भी जुड़े रहे, इसलिए उनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है तथा शब्दावली भी वह है जो आम आदमी पढ़ता, लिखता और बोलता है। नूर साहब के तीनों ग़ज़ल-संग्रहों - (1) "दुख-सुख", (2) "तपस्या", और (3) "समन्दर मेरी तलाश में है", के नाम इस बात का प्रमाण हैं कि वे हिन्दी के अधिक निकट रहे। चूँकि 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में पैदा हुए लोगों का मुख्य रूप से दो ही भाषाओं- उर्दू और अंग्रेज़ी- से सामना हुआ। इसलिए नूर साहब भी विशेष रूप से उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़े। उनके लिखने का प्रवाह भी पर्सियन लिपि में अधिक था।
उनके प्रथम ग़ज़ल-संग्रह 'दुख-सुख' की ग़ज़लों में उर्दू-फ़ारसी शब्दों की अधिकता है, जबकि दूसरे ग़ज़ल-संग्रह 'तपस्या' में उनकी भाषा काफ़ी सरल हुई। तीसरे ग़ज़ल-संग्रह 'समन्दर मेरी तलाश में है' में तो उन्होंने उर्दू और हिन्दी का अन्तर ही समाप्त कर दिया। इस संग्रह की ग़ज़लें हिन्दी एवं हिन्दुस्तानी भाषा में हैं। ऐसा नहीं कि नूर साहब ने उर्दू-साहित्य की सेवा नहीं की। उर्दू-साहित्य की उन्होंने भरपूर सेवा की। इस बात का प्रमाण उर्दू अकादमी द्वारा उन्हें दिया गया 51,000 रुपये का पुरस्कार एवं कई अन्य पुरस्कार एवं सम्मान हैं। लेकिन, अपने 'भारतीयपन', 'पौराणिक चिन्तन' और 'हिन्दीपन' के कारण वे उर्दू समालोचकों को रुचे नहीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि नूर साहब के काव्य में राष्ट्रीयता की स्थापना है। फिर उर्दू का जन्मदाता भारत है, इसलिए उसका सीधा सम्बन्ध यहाँ की संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र आदि से है, जिसमें तमाम तरह के दर्शन, धार्मिक विश्वास और सह-अस्तित्व के तत्व शामिल हैं।
उर्दू समालोचकों द्वारा की गयी यह कोताही ही सम्भवतः नूर साहब को हिन्दी की ओर खींच लायी। नूर साहब स्वयं इस बात को स्वीकारते थे कि वह आम आदमी के नहीं, बल्कि उन लोगों के कवि हैं, जिनमें सोचने, समझने और परखने की क्षमता है। यक़ीनन बुद्धिजीवी वर्ग ने हमेशा उनको सर-आँखों पर बिठाये रखा। वह कवियों के कवि बनकर रहे। आज भी नूर साहब के शेर लोगों में नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी।
नूर साहब की ग़ज़लों का वण्र्य-विषय मुख्य रूप से अध्यात्म और श्रंगार है। लेकिन उनके कथ्य की यह विशेषता है कि अध्यात्म में शृंगार और शृंगार में अध्यात्म के दर्शन होते हैं। उनके शृंगार में सौन्दर्य की परम्परागत मांसलता नहीं, बल्कि सौन्दर्य की आत्मा निवास करती है। उन्होंने कभी भारतीय दर्शन की उँगली नहीं छोड़ी, यही कारण है कि उनका साहित्य-संसार उनकी कल्पनाओं की ही तरह सुघड़ और असीम है। अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों एवं संस्कृत की वह तत्सम शब्दावली जिसे हिन्दी गीतकार भी प्रयोग करने में संकोच करते हैं, नूर साहब ने उस शब्दावली को शेरों में लाकर यह सिद्ध कर दिया कि शब्द चाहे किसी भी भाषा का हो, उसको प्रयोग करने का ढंग रचनाकार के पास होना चाहिए।
उन्होंने नमन, हवन, कार्य, दूभर, ज्वाला, शमन, हृदय, इच्छा, दमन, साधना, तपस्या, अन्त, गहन संध्या, रूप, पूजा, नयन, आशंका, पर्वत, शिखर, आस्था, गंगाजल, आचमन, मार्गदर्शक, आयतन, दुख-सुख, लज्जित, आराधना, आवश्यक, जीवन, कामिनी, मन, नूपुर, वंदना, राजपथ, संकेत, चि“न, चल-अचल, आकाश, धरती, अस्तित्व, दिशा, आरम्भ, ध्यान, वर्णन, शब्द, भाषा, मीरा, अधिकार, साधू, गेरुए, खटपट, जनम, बूँद, अमृत, चन्दन, सिन्दूर, सुहागन, साधना, माँग, चुनाव, आवागमन, धरती, देवता, मन्दिर, मिलन, तपस्या, ईश्वर, बधाई, ध्यान, अन्तिम, पृष्ठ, नाविल, राम, अस्तित्व, सीता, विशाल, सूरज, खँडर, बेला, अर्थहीन, पुस्तक, लक्ष्मण-रेखा, धरना, भाषा, कंकर, गागर, कारण, अता-पता, धन, अवतार, रचना, पतवार, गंगा, सचित्र, चरित्र, पवित्र, विचित्र, चित्र, मित्र, धर्म, मुखड़ा, दरपन, पाप, आदर्श, ममता, रक्षक, भक्षक, जननी, अन्तर्दृष्टि, दर्शन, बिंदिया, हे हंसवाहिनी, वरदान, माँ दुर्गा, वाणी, शब्द, अर्थ, सुगन्ध, ज्ञान, चरण, अरपन, भगवती, भिखारन, हे सिंहवाहिनी, महिषासुर, कष्ट, मुक्ति, जगदम्बे, विनती, निवेदन, शंकर, तिरशूल, अवतार, ओर, कमरे आदि संस्कृत और हिन्दी के तथा नाविल व फ़्रेम जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अपनी ग़ज़लों में करके हिन्दी ग़ज़लकारों के लिए रास्ता तैयार कर दिया है।
नूर साहब ने अपनी ग़ज़लों में प्रतीक और बिम्ब भी भारतीय दर्शन से लिये हैं। उनके प्रतीकों और बिम्बों में गीता, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण आदि की गन्ध आती है। उनके यहाँ परम्परागत ज्ञान, कल्पना और आदर्श को नये यथार्थ से जोड़कर कहने की परिपाटी मौजूद है। वे नये बिम्बों का प्रयोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। 'नींद से आँखों की खटपट', 'दुख-सुख की कसौटी', 'अनदेखे उजाले की दीवार', 'तपे हुए खरे सोने का भाव', 'देवता की तरह मन्दिर में क़ैद होना', 'आवाज़ की छुअन', 'ध्यान में गुम', नाविल में 'अन्तिम पृष्ठ', 'मिलन की बेला', ज़िन्दगी के लिए 'पिछले जनम की गाढ़ी कमाई', 'अर्थहीन-सी पुस्तक', मन्दिर का दीया, 'धूप-छाँव', 'सूरजमुखी का फूल' व 'माँ द्वारा बच्चे को उछालकर खिलाना', राजपथ पर 'संकेतों के चिह्न', साँसों का 'दुख को नमन', आँखों द्वारा 'रूप की पूजा', 'आशंकाओं के पर्वत-शिखर', 'आस्था का गंगाजल', 'क़दों का आयतन', 'आराधना में ग़बन', 'साँसों की लक्ष्मण-रेखा', दर्पण को 'सोने के फ़्रेममें जड़ना', 'ओस की उँगलियाँ', 'ज़िन्दगी के पुराने शुमारे', 'रोशनी का शोर', चिता के धुएँ के लिए 'आग के क़लम की सियाही', बिंदिया के लिए 'मन्दिर का चिराग़', होंठों के लिए 'खिलता हुआ फूल', आँसुओं के लिए 'यादांे के दीये', ग़मों के लिए 'नागन', सच्चे प्यार के लिए 'चन्दन' आदि प्रतीकों और बिम्बों का सटीक और सुन्दर प्रयोग उनकी ग़ज़लों में मिलता है, जो भारतीय संस्कृति में सराबोर हैं। उन्होंने यह बता दिया और जता दिया कि हिन्दी ग़ज़ल में असीम सम्भावनाएँ छिपी हैं। हिन्दी ग़ज़ल वास्तविकता के धरातल पर पाँव जमाये हुए है, उसमें कोरी कल्पनाएँ नहीं हैं।
जहाँ तक पूर्ववर्ती काव्य-परम्परा के प्रभाव का प्रश्न है, तो प्रत्येक रचनाकार अपने अग्रजों से कुछ न कुछ सीखता है। नूर साहब ने भी अपने पूर्ववर्तियों और वरिष्ठ रचनाकारों से विचार ग्रहण किये हैं और अपने प्रभावशाली कथ्य के द्वारा सुन्दर अभिव्यक्ति भी दी है। नूर साहब ने स्वयं अपने ग़ज़ल-संग्रह 'समन्दर मेरी तलाश में है' में 'साफ़-साफ़' शीर्षक के अन्तर्गत अन्य कवियों-शायरों के शेरों के साथ अपने शेर उद्धृत करते हुए लिखा है कि मैंने इन चिराग़ों से चिराग़ जलाये हैं। लेकिन नूर साहब ने अपने शेरों को 'फ़ारसीपन' से मुक्त कर 'हिन्दीपन' से सराबोर कर दिया है। नूर साहब का प्रभाव भी परवर्ती ग़ज़लकारों पर पड़ा है। बहुत से ग़ज़लकार उनकी साफ़-सुथरी शैली को अपनाकर अपनी साहित्यिक यात्रा जारी रखे हुए हैं।
बीसवीं शताब्दी में काव्य-यात्रा आरम्भ करने वाले नूर साहब की रचनाधर्मिता ने 21वीं शताब्दी को भी प्रभावित किया है। उन्होंने अपना दो सदियों का ज्ञान और चिन्तन अपनी हिन्दी ग़ज़लों के माध्यम से परवर्तियों को सौंपा है। उनके यहाँ महर्षि परम्परा द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक चिन्तन के पुष्प नये रंगों और नयी गन्धों के साथ खिले हुए मिलते हैं। जीवन की पीड़ाओं की अमावस्या में नूर साहब के विचार दीपावली के दीपों की तरह झिलमिलाते हैं। जहाँ बुद्धि के देवता का गणेशत्व और कलात्मक चिन्तन की महालक्ष्मी श्रद्धा के साथ विराजमान रहती हैं और व्यक्ति की चेतना उनका नमन करने में जीवन की सार्थकता महसूस करती है। वह ध्यान की ख़ुशबू में इस प्रकार निमग्न हो गये हैं कि भाषा और शब्द मौन ओढ़कर उनके सम्मुख जड़वत् खड़े हैं। उन्होंने साहित्य-सृजन के लिए जो रंग चुना, सारे रंग उस रंग के सामने फीके पड़ जाते हैं। अपने चिन्तन के द्वारा लोकप्रियता के उस शिखर को छुआ, जहाँ प्रसिद्धि विलुप्त हो जाती है और यश आरम्भ हो जाता है। उन्होंने अपने काव्यात्मक-उद्यान को आस्था के गंगाजल से इस प्रकार सींचा है कि सारी आशंकाएँ धूल बनकर उड़ जाती हैं और नवीन सम्भावनाओं की मीठी और मस्त ख़ुशबू सभी दिशाओं को सुगन्धित कर देती है। अपनी रचनाओं के बीच नूर साहब सन्त की भूमिका में दिखायी देते हैं।
नूर साहब की यही विशेषता उन्हें हिन्दी ग़ज़लकारों की बेतरतीब बढ़ती भीड़ से अलग ऐसे ऊँचे सिंहासन पर आसीन करती है, जहाँ भारत है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, भारतीय चिन्तन है और भारतीय परिवेश है। उनकी ग़ज़ल की देवी इन्हीं सब परिधानों को धारण कर हिन्दी ग़ज़ल की असीम सम्भावनाओं के लिए द्वार खोल देती है।
डा. कृष्णकुमार 'नाज़'
उनके प्रथम ग़ज़ल-संग्रह 'दुख-सुख' की ग़ज़लों में उर्दू-फ़ारसी शब्दों की अधिकता है, जबकि दूसरे ग़ज़ल-संग्रह 'तपस्या' में उनकी भाषा काफ़ी सरल हुई। तीसरे ग़ज़ल-संग्रह 'समन्दर मेरी तलाश में है' में तो उन्होंने उर्दू और हिन्दी का अन्तर ही समाप्त कर दिया। इस संग्रह की ग़ज़लें हिन्दी एवं हिन्दुस्तानी भाषा में हैं। ऐसा नहीं कि नूर साहब ने उर्दू-साहित्य की सेवा नहीं की। उर्दू-साहित्य की उन्होंने भरपूर सेवा की। इस बात का प्रमाण उर्दू अकादमी द्वारा उन्हें दिया गया 51,000 रुपये का पुरस्कार एवं कई अन्य पुरस्कार एवं सम्मान हैं। लेकिन, अपने 'भारतीयपन', 'पौराणिक चिन्तन' और 'हिन्दीपन' के कारण वे उर्दू समालोचकों को रुचे नहीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि नूर साहब के काव्य में राष्ट्रीयता की स्थापना है। फिर उर्दू का जन्मदाता भारत है, इसलिए उसका सीधा सम्बन्ध यहाँ की संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र आदि से है, जिसमें तमाम तरह के दर्शन, धार्मिक विश्वास और सह-अस्तित्व के तत्व शामिल हैं।
उर्दू समालोचकों द्वारा की गयी यह कोताही ही सम्भवतः नूर साहब को हिन्दी की ओर खींच लायी। नूर साहब स्वयं इस बात को स्वीकारते थे कि वह आम आदमी के नहीं, बल्कि उन लोगों के कवि हैं, जिनमें सोचने, समझने और परखने की क्षमता है। यक़ीनन बुद्धिजीवी वर्ग ने हमेशा उनको सर-आँखों पर बिठाये रखा। वह कवियों के कवि बनकर रहे। आज भी नूर साहब के शेर लोगों में नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी।
नूर साहब की ग़ज़लों का वण्र्य-विषय मुख्य रूप से अध्यात्म और श्रंगार है। लेकिन उनके कथ्य की यह विशेषता है कि अध्यात्म में शृंगार और शृंगार में अध्यात्म के दर्शन होते हैं। उनके शृंगार में सौन्दर्य की परम्परागत मांसलता नहीं, बल्कि सौन्दर्य की आत्मा निवास करती है। उन्होंने कभी भारतीय दर्शन की उँगली नहीं छोड़ी, यही कारण है कि उनका साहित्य-संसार उनकी कल्पनाओं की ही तरह सुघड़ और असीम है। अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों एवं संस्कृत की वह तत्सम शब्दावली जिसे हिन्दी गीतकार भी प्रयोग करने में संकोच करते हैं, नूर साहब ने उस शब्दावली को शेरों में लाकर यह सिद्ध कर दिया कि शब्द चाहे किसी भी भाषा का हो, उसको प्रयोग करने का ढंग रचनाकार के पास होना चाहिए।
उन्होंने नमन, हवन, कार्य, दूभर, ज्वाला, शमन, हृदय, इच्छा, दमन, साधना, तपस्या, अन्त, गहन संध्या, रूप, पूजा, नयन, आशंका, पर्वत, शिखर, आस्था, गंगाजल, आचमन, मार्गदर्शक, आयतन, दुख-सुख, लज्जित, आराधना, आवश्यक, जीवन, कामिनी, मन, नूपुर, वंदना, राजपथ, संकेत, चि“न, चल-अचल, आकाश, धरती, अस्तित्व, दिशा, आरम्भ, ध्यान, वर्णन, शब्द, भाषा, मीरा, अधिकार, साधू, गेरुए, खटपट, जनम, बूँद, अमृत, चन्दन, सिन्दूर, सुहागन, साधना, माँग, चुनाव, आवागमन, धरती, देवता, मन्दिर, मिलन, तपस्या, ईश्वर, बधाई, ध्यान, अन्तिम, पृष्ठ, नाविल, राम, अस्तित्व, सीता, विशाल, सूरज, खँडर, बेला, अर्थहीन, पुस्तक, लक्ष्मण-रेखा, धरना, भाषा, कंकर, गागर, कारण, अता-पता, धन, अवतार, रचना, पतवार, गंगा, सचित्र, चरित्र, पवित्र, विचित्र, चित्र, मित्र, धर्म, मुखड़ा, दरपन, पाप, आदर्श, ममता, रक्षक, भक्षक, जननी, अन्तर्दृष्टि, दर्शन, बिंदिया, हे हंसवाहिनी, वरदान, माँ दुर्गा, वाणी, शब्द, अर्थ, सुगन्ध, ज्ञान, चरण, अरपन, भगवती, भिखारन, हे सिंहवाहिनी, महिषासुर, कष्ट, मुक्ति, जगदम्बे, विनती, निवेदन, शंकर, तिरशूल, अवतार, ओर, कमरे आदि संस्कृत और हिन्दी के तथा नाविल व फ़्रेम जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अपनी ग़ज़लों में करके हिन्दी ग़ज़लकारों के लिए रास्ता तैयार कर दिया है।
नूर साहब ने अपनी ग़ज़लों में प्रतीक और बिम्ब भी भारतीय दर्शन से लिये हैं। उनके प्रतीकों और बिम्बों में गीता, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण आदि की गन्ध आती है। उनके यहाँ परम्परागत ज्ञान, कल्पना और आदर्श को नये यथार्थ से जोड़कर कहने की परिपाटी मौजूद है। वे नये बिम्बों का प्रयोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। 'नींद से आँखों की खटपट', 'दुख-सुख की कसौटी', 'अनदेखे उजाले की दीवार', 'तपे हुए खरे सोने का भाव', 'देवता की तरह मन्दिर में क़ैद होना', 'आवाज़ की छुअन', 'ध्यान में गुम', नाविल में 'अन्तिम पृष्ठ', 'मिलन की बेला', ज़िन्दगी के लिए 'पिछले जनम की गाढ़ी कमाई', 'अर्थहीन-सी पुस्तक', मन्दिर का दीया, 'धूप-छाँव', 'सूरजमुखी का फूल' व 'माँ द्वारा बच्चे को उछालकर खिलाना', राजपथ पर 'संकेतों के चिह्न', साँसों का 'दुख को नमन', आँखों द्वारा 'रूप की पूजा', 'आशंकाओं के पर्वत-शिखर', 'आस्था का गंगाजल', 'क़दों का आयतन', 'आराधना में ग़बन', 'साँसों की लक्ष्मण-रेखा', दर्पण को 'सोने के फ़्रेममें जड़ना', 'ओस की उँगलियाँ', 'ज़िन्दगी के पुराने शुमारे', 'रोशनी का शोर', चिता के धुएँ के लिए 'आग के क़लम की सियाही', बिंदिया के लिए 'मन्दिर का चिराग़', होंठों के लिए 'खिलता हुआ फूल', आँसुओं के लिए 'यादांे के दीये', ग़मों के लिए 'नागन', सच्चे प्यार के लिए 'चन्दन' आदि प्रतीकों और बिम्बों का सटीक और सुन्दर प्रयोग उनकी ग़ज़लों में मिलता है, जो भारतीय संस्कृति में सराबोर हैं। उन्होंने यह बता दिया और जता दिया कि हिन्दी ग़ज़ल में असीम सम्भावनाएँ छिपी हैं। हिन्दी ग़ज़ल वास्तविकता के धरातल पर पाँव जमाये हुए है, उसमें कोरी कल्पनाएँ नहीं हैं।
जहाँ तक पूर्ववर्ती काव्य-परम्परा के प्रभाव का प्रश्न है, तो प्रत्येक रचनाकार अपने अग्रजों से कुछ न कुछ सीखता है। नूर साहब ने भी अपने पूर्ववर्तियों और वरिष्ठ रचनाकारों से विचार ग्रहण किये हैं और अपने प्रभावशाली कथ्य के द्वारा सुन्दर अभिव्यक्ति भी दी है। नूर साहब ने स्वयं अपने ग़ज़ल-संग्रह 'समन्दर मेरी तलाश में है' में 'साफ़-साफ़' शीर्षक के अन्तर्गत अन्य कवियों-शायरों के शेरों के साथ अपने शेर उद्धृत करते हुए लिखा है कि मैंने इन चिराग़ों से चिराग़ जलाये हैं। लेकिन नूर साहब ने अपने शेरों को 'फ़ारसीपन' से मुक्त कर 'हिन्दीपन' से सराबोर कर दिया है। नूर साहब का प्रभाव भी परवर्ती ग़ज़लकारों पर पड़ा है। बहुत से ग़ज़लकार उनकी साफ़-सुथरी शैली को अपनाकर अपनी साहित्यिक यात्रा जारी रखे हुए हैं।
बीसवीं शताब्दी में काव्य-यात्रा आरम्भ करने वाले नूर साहब की रचनाधर्मिता ने 21वीं शताब्दी को भी प्रभावित किया है। उन्होंने अपना दो सदियों का ज्ञान और चिन्तन अपनी हिन्दी ग़ज़लों के माध्यम से परवर्तियों को सौंपा है। उनके यहाँ महर्षि परम्परा द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक चिन्तन के पुष्प नये रंगों और नयी गन्धों के साथ खिले हुए मिलते हैं। जीवन की पीड़ाओं की अमावस्या में नूर साहब के विचार दीपावली के दीपों की तरह झिलमिलाते हैं। जहाँ बुद्धि के देवता का गणेशत्व और कलात्मक चिन्तन की महालक्ष्मी श्रद्धा के साथ विराजमान रहती हैं और व्यक्ति की चेतना उनका नमन करने में जीवन की सार्थकता महसूस करती है। वह ध्यान की ख़ुशबू में इस प्रकार निमग्न हो गये हैं कि भाषा और शब्द मौन ओढ़कर उनके सम्मुख जड़वत् खड़े हैं। उन्होंने साहित्य-सृजन के लिए जो रंग चुना, सारे रंग उस रंग के सामने फीके पड़ जाते हैं। अपने चिन्तन के द्वारा लोकप्रियता के उस शिखर को छुआ, जहाँ प्रसिद्धि विलुप्त हो जाती है और यश आरम्भ हो जाता है। उन्होंने अपने काव्यात्मक-उद्यान को आस्था के गंगाजल से इस प्रकार सींचा है कि सारी आशंकाएँ धूल बनकर उड़ जाती हैं और नवीन सम्भावनाओं की मीठी और मस्त ख़ुशबू सभी दिशाओं को सुगन्धित कर देती है। अपनी रचनाओं के बीच नूर साहब सन्त की भूमिका में दिखायी देते हैं।
नूर साहब की यही विशेषता उन्हें हिन्दी ग़ज़लकारों की बेतरतीब बढ़ती भीड़ से अलग ऐसे ऊँचे सिंहासन पर आसीन करती है, जहाँ भारत है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, भारतीय चिन्तन है और भारतीय परिवेश है। उनकी ग़ज़ल की देवी इन्हीं सब परिधानों को धारण कर हिन्दी ग़ज़ल की असीम सम्भावनाओं के लिए द्वार खोल देती है।
डा. कृष्णकुमार 'नाज़'
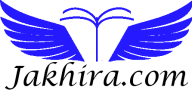




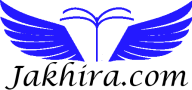





COMMENTS