आधुनिक शायरी में जनजीवन - डॉ. कृष्ण कुमार नाज़ स्वर्गीय नूर साहब का यह मज़मून उनके प्रिय शिष्य डॉ. कृष्ण कुमार 'नाज़' ने हमें उपलब्ध कराया, जो उर्दू में
आधुनिक शायरी में जनजीवन - डॉ. कृष्ण कुमार नाज़
स्वर्गीय नूर साहब का यह मज़मून उनके प्रिय शिष्य डॉ. कृष्ण कुमार 'नाज़' ने हमें उपलब्ध कराया, जो उर्दू में नूर साहब की हस्तलिपि में था। नूर साहब ने ज़िंदगी-भर शायरी की और मुशायरे पढ़े, नस्र (गद्य) में बाक़ायदा कभी कुछ नहीं लिखा। हमने पूरे मज़मून को यहाँ ज्यों का त्यों इसलिए लिया है कि पढ़ने वालों को कम से कम इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि नूर साहब राजनीति, समाज और मुशायरों के बारे में अपनी क्या सोच रखते थे। - देवेन्द्र गेहलौददुनिया की सब ही जु़बानों के अदब में अदीबों और शायरों ने अपने अह्द यानी अपने ज़माने की अवामी ज़िंदगी को बहुत ही मुअस्सर अंदाज़ में हमेशा ही पेश किया है। अदब की कोई भी सिन्फ़ क्यों न हो, सब ही में अवाम की ज़िंदगी की गूंज ज़रूर होती है। शायरी चूंकि बहुत ही नर्म और नाज़ुक अहसासात को अल्फ़ाज का जामा देने का जामेअ काम करती है। यही वजह है कि चंद लफ़्ज़ों में हयात के मुख़्तलिफ़ पहलुओं को बड़ी आसानी और कामयाबी के साथ अवाम के अहसासात को अवाम के सामने पेश कर देती है। गुज़रे ज़माने में भी अदब अवाम से जुड़ा रहा जिसके सुबूत में प्रेमचंद की कहानियां और अफ़साने रखे जा सकते हैं। वह गोदान हो, दो बीघा जमीन हो या कोई भी कहानी हो। ग़ालिब भी समाज से अलग न रह सके।
बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता
वगरना शह्र में 'ग़ालिब' की आबरू क्या है
मगर यहां तो हमें अपने अह्द के बारे में बात करना है। यह देखना है कि इस युग में क्या हो रहा है? 'ख़ुमार' साहब को ही ले लीजिए जो आज के हर दिल अज़ीज और मकबूल शायर हैं। पूरी शायरी जज़्बातो-ख़यालात, हुस्नो-इश्क़ में ग़र्क़ मिलती है, मगर उन्होंने भी एक मुक़ाम पर जो कर्ब महसूस किया, वह कुछ इस तरह नज़्म कर दिया-
चि़रागों के बदले मक़ां जल रहे हैं
नया है ज़माना, नई रोशनी है
यूं तो किसी शेर से कभी यह नहीं ज़ाहिर होता कि शेर शायर ने किसी मजबूरी के तहत कहा है या उसको किसी दबाव में रहकर लिखना पड़ा है, मगर यहां असल बात यह है कि अदीब या शायर जो ज़िंदगी जीता है या अपने चारों तरफ जो फ़िज़ा उसे मिलती है या जिस तरह दूसरों को जीते देखता है, वही सब कुछ तो वह चंद लफ़्ज़ों में समेटकर शेर की सूरत में ढाल देता है। हां, एक ज़माना था जब शायरी अवाम से बराए-नाम वास्ता रखती थी। इस ज़माने से मुराद सौ, दो सौ, चार सौ साल नहीं, यही कोई पचास-साठ साल पहले तक जब रियासतें क़ायम थीं, रजवाड़े ख़त्म नहीं हुए थे। ज़मींदारों और रईसों की एक अलग दुनिया थी, तब शायर का फ़न उन्हीं लोगो की क़द्रदानी का मुहताज था। शायरी का तआरुफ़ उन लोगों से था जिन्हें सोसायटी में ख़वास का दर्जा हासिल था और सच पूछिये तो वे लोग फ़न के पारखी भी हुआ करते थे।
शायरों को ख़लअतें, इनामात, जागीरें और दीगर अतियात से जब तब नवाज़ते रहते थे। मगर जब वह सब कुछ एक ख़्वाब हो गया तो शायरी भी अपने अस्तित्व (ज़िंदगी) के लिए दरबारों से निकलकर बाज़ारों में आ गई और फिर इसके लिए लाज़िम हो गया कि वह अपनी बक़ा के लिए अवाम से जुड़ी रही। ज़ाती मुआमलात से क़ते-नज़र शायरी अवाम के दरमियान आई तो उसके मौजू़-ए-सुख़न भी वे न रहे कि जो थे। कहां वे ऐशो-आराम तफ़रीह, आसूदगी, अमीरी और मुसर्रतों के माहौल में सांसें लेती थी। कहां भूख, बेकारी, दुख, उलझन, घुटन, कर्ब और महरूमी के मंज़रों में कै़द हो गई। यहां उसे मज़हबी, सियासी और समाजी मसाइल अपने में उलझा लिया। फिर शायरी को भी आला क़द्रों की जानिब निगाह करनी पड़ी।
इन दिनों तालीम के सिलसिले में जो बेदारी हमारी हुकूमत की काविश से अवाम में आई है, उसकी वजह से भी और कुछ रेडियो और टी.वी. की मक़बूलियत के सबब जो सियासी शऊर हासिल हुआ, उसके नतीजे में अवाम भी सियासत में ख़ासी दिलचस्पी लेने लगे। आपको याद होगा जब हम आज़ाद हुए थे, खादी को और खादी पहनने वाले को कितनी मुहतरम और पाकीज़ा निगाहों से देखा जाता था। बताने की जरूरत नहीं कि आज पचास साल बाद उसी खादी और खादी पहनने वालों को किस निगाह से देखा जाता है। इसी कुर्ब को इस शेर में देखा जा सकता है-
इस अह्द का वो सबसे बड़ा मोजज़ा बने
खद्दर पहन के कोई जो सच बोलने लगे
और सुनिए-
क्या दिलकशी ग़ज़ब की सियासत दुल्हन में है
लीडर का दिल भी जु़ल्फ़े-शिकन-दर-शिकन में है
मुलाहज़ा हो-
काजू भुने प्लेट में, व्हिस्की गिलास में
आया है रामराज विधायक निवास में
अवाम का सियासी लोगों के बारे में क्या ख़याल है, इस जानिब भी एक शायर ने इशारा किया है-
हाथ तो बेशक मिलाएं हर सियासतदां से आप
लेकिन उसके बाद अपनी उंगलियां गिन लीजिए
ये सारे ख़यालात लाज़िमो-मलज़ूम से हो गए हैं, क्योंकि-
सियासत और उजला पैरहन एक साथ नामुमकिन
वहां तक जाने वाले रास्ते दलदल के होते हैं
सियासी हवाले से गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म न समझी जाए। अगर तमाम शायरों के तमाम अशआर यकजा किए जाएं, तो शायद एक किताब तैयार हो जाये। अब आइए उस तरफ चलें जहां एक आम इंसान अपने मज़हब से पूरी तरह जुड़ा है और ग़ैर मज़हब के इंसानों के दरमियान ज़िंदगी गुज़ार रहा है। यूं तो हमारे मुल्क में बहुत से मज़हब हैं। मैं यहां सिर्फ़ दो ख़ास मज़हब के लोगों के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहूंगा। एक है हिंदू और एक है मुसलमान। एक ज़माना था जब शायरी के बहाने एक-दूसरे पर तंज़ किया जाता था और उसका जवाब भी बड़े मुहज़्ज़ब पैराए में शेर ही के ज़रिये दिया जाता था। पंडित दयाशंकर 'नसीम' को एक मिसरे पर मिसरा लगाने को कहा गया। मिसरा था-
शेख़ ने मस्जिद बना मिसमार बुतख़ाना किया।
ज़ाहिर है बुतपरस्ती या मूर्ति पूजा पर यह खुली चोट थी, मगर वाह, पंडित जी ने मिसरा लगा कर इस चिंगारी को यूं ख़ाक में दफ़्न कर दिया कि-
तब तो कुछ सूरत भी थी, अब साफ़ वीराना किया।
इस क़िस्म की इल्मी नोकझोक का कभी कोई रद्दे-अमल अवाम में न होता और बात तफ़रीह की हदों से आगे न बढ़ा करती थी, मगर इस अह्द में हमारे रहबरों ने और कुछ जाहिल सियासतदानों ने अपनी चालों से हिंदू-मुसलमान दोनों को एक-दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया, जो फ़सादात की शक्ल में मंज़रे-आम पर नुमायां होते रहे हैं। मुंबई के ताज़ा फ़सादात की रोशनी में एक शायर ने बड़ा ही गंदा शेर कह डाला, जिसे अवाम ने ख़ूब सराहा, मगर बाद में जब उस शेर पर ग़ौर किया तो ख़ुद ही शर्मिंदा भी हुए। शेर सिर्फ़ याददाश्त के बल पर लिख रहा हूं। अल्फ़ाज़ की नशिस्त में तो फ़र्क़ हो सकता है, मगर मफ़हूम में नहीं-
बेगुनाहों पे अगर यूं ही सितम तोड़ोगे
फिर तो हर बच्चा मेरी क़ौम का मेमन होगा
एक शायर ने अपने ज़ाती जज़बात की यूं नुमाइंदगी की-
हमें भी हौसला दे गज़नवी का
मुसलसल हार से तंग आ गए हैं
और एक शायर ने तो यहां तक कह दिया-
अपने काबे की हिफ़ाज़त हमें ख़ुद करनी है
अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला
चलते-चलते एक और शेर सुन लें, जिसमें हुकूमत के नशे की बात को उजागर किया गया है-
हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज़ न कर
हमारे ताज अजायबघरों में रक्खे हैं
ख़ैर साहब ऐसा नहीं कि इस मज़हबी मंज़रनामे पर सिर्फ़ आग ही आग बरसती हो, कुछ शायरों ने शबनम का छिड़काव भी किया। ये अलग बात कि आग लग जाए तो उसके फैलने में देर नहीं लगती। उसको बुझाने में काफ़ी वक्त लग जाता है-
आग का क्या है पल दो पल में लगती है
बुझते-बुझते एक ज़माना लगता है
इस मौज़ू पर कुछ शेर हाज़िर हैं। क़ौमी यकजहती की मिसाल-
कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे
परिंदों में कोई फ़िरक़ापरस्ती क्यों नहीं होती
या फिर एक और सोच-
जिसके कारण फ़साद होते हैं
उसका कोई अता-पता ही नहीं
एक और सेहतमंद फ़िक्र-
रहे-दैर हो कि रहे-हरम,
मगर एक दोनों की मंज़िलें
ये तो अपनी-अपनी निगाह थी,
कुछ इधर गए, कुछ उधर गए
एक मुक़ाम पर इसी उनवान को ज़ेहन (दिमाग) में रखते हुए यूं भी शायर ने कहा-
शह्र जलने का है सबब ये भी
लोग इक-दूसरे से जलते हैं
मेरा ख़याल है, इस बारूदी मसअले को यहीं छोड़ दिया जाए, वरना दीगर अहम गोशों पर ठीक से रोशनी न पड़ सकेगी। अब एक निगाह अवाम की ज़िंदगी के दूसरे पहलू पर भी डाल ली जाए। बीते दिनों में आपस में इतने मुख़्तलिफ़ ख़यालात न थे, जितने आज हैं। समाज सुधार के उसूल तो तराशे गए, मगर उन पर अमल हुआ ही नहीं। यानी हर क़िस्म के भेदभाव को ख़त्म हो जाने का मौक़ा तो फ़राहम हुआ, मगर इससे फ़ायदा पूरी तरह न उठा सके। बसों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाले ने ये कब सोचा कि वो किस क़ौम के फ़र्द के पहलू में बैठा हुआ सफ़र कर रहा है, बराबर वाली नशिस्त पर कौन है।
ऐसा तो नहीं कि हम जो सांस ले रहे हैं, वो किसी अछूत के मुंह से निकली हुई हवा हो या जिसके हाथ से हम पानी लेकर पी रहे हैं, वह किस तबक़े से तअल्लुक़ रखता है, ये कभी सोचा है। दौराने-सफ़र जो खाना हमको मयस्सर होता है, उसको पकाने वाला कौन है। ये सवाल कभी ज़ह्न में आता है? हम सब भूल गए, ज़ात-पात के भेदभाव के धुंधले नक़ूश भी इस तवील अरसे में नहीं मिलते (आज़ादी के बाद से आज तक) मगर हमारे सियासतदां तफ़रीक बरतने से नहीं चूकते। रिज़र्वेशन की आड़ में ख़ुदा मालूम क्या-क्या गुल खिलाए चले जा रहे हैं, जिसके सुबूत अक्सर और बेशतर सामने आते रहे हैं।
सबके दिल में प्यार का अरमान बन कर जी सकूं
मुश्किलों में भी कभी आसान बन कर जी सकूं
मुझसे मेरी ज़ात, मज़हब, नाम सब कुछ छीन लो
जिससे मैं इंसान, बस इंसान बन कर जी सकूं
समाजी लानत या समाजी बुराई के दायरे में एक अहम मसला दहेज़ का भी है। समाजी जिं़दगी इस ग़ैर मज़हबी रस्म से काफ़ी दुखी और आजिज़ है। हर इंसान एक अजीब-सी घुटन का शिकार है। कहीं लड़कियां ख़ुदकुशी कर रही हैं, कहीं दुल्हनें जलाई जा रही है, कहीं वालिदैन ज़िंदगी से फ़रार हासिल करने की फ़िक्र में डूबे मिलते हैं।
वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र
ज़ंजीर खींच कर जो मुसाफ़िर उतर गया
ज़िंदगी की तल्ख़ियां अब कौन-सी मंज़िल पे हैं
इससे अंदाज़ा लगा लो ज़ह्र महंगा हो गया
आने वाले दिन मसाइल ले के आएंगे 'बशीर'
घर के आंगन में कई चेह्रे जवां हो जाएंगे
एक शायरा ने इस कर्ब का इज़हार यूं किया-
अह्ले-दुनिया चाहे जो समझें, उन्हें है इख़्तियार
ज़िंदगी उस मोड़ पर थी, ख़ुदकुशी अच्छी लगी
इस दहेज़ की बदौलत मियां-बीवी के माबैन तलाक़ तक बात पहुंची तो एक शेर ने जन्म ले ही लिया-
तलाक़ दे तो रहे हो ग़ुरूरो-कहर के साथ
मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ
आजकल समाजी ज़िंदगी में ज़िंदगी की कुछ अहम क़द्रें तबाह हो गईं या तबाह हो रही हैं, इस अमल को भी नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से एक इंसान रिश्तों की जिस डोर से बंधा है, वो डोर अब ढीली पड़ती जा रही है। वो चाहे बाप-बेटे का रिश्ता हो या मियां-बीवी का। इस कर्ब को यूं कहा गया-
मां की सांस, पिता की खांसी
सुनते थे जो कान नहीं हैं
लोग रिश्तों की डोर थामे हुए
साथ चलते हैं, फ़ासला है बहुत
ये भी शेर मुलाहिज़ा हो-
मैं चाहती थी उसको बचा लूं किसी तरह
अफ़सोस मुझको लोगों ने क़ातिल समझ लिया
अब एकाध शेर जिनमें शायर ने बड़े धीमे लह्जे में ग़ायब होती हुई क़दरों की तरफ़ इशारा किया है देखें। ज़रा अह्द का कर्ब देखें-
हम अपने अह्द की ख़ुशियां ख़रीदते कैसे
हमारे पास गुज़िश्ता सदी के सिक्के थे
एक और शेर हाज़िर है-
वो चंद क़दरें जो तहज़ीब की बची हैं उन्हें
छुपाए फिरता हूं इक्कीसवीं सदी के लिए
एक और ख़ूबसूरत हक़ीक़त-
मुस्कराहट, सादगी, लह्जा, ख़ुलूस
बेचकर मैं सारे ज़ेवर खा गया
या फिर-
लौटा सज़ा जो काट के नाकरदा जुर्म की
घर आके उसने सारे परिंदे रिहा किए
हां साहब, बेकारी भी आम ज़िंदगी में एक बड़ा ही अहम मसला है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसका कारण आप कुछ समझें, मगर मेरे ख़याल में ये रोज़-ब-रोज़ बढ़ती हुई आबादी ही है कि लोग तलाशे-मआश में देहात से बड़े-बड़े शह्रों की तरफ़ भागने लगे या तिजारत के ख़याल से गांव छोड़ कर शह्रों की जानिब उमड़ने लगे। शह्र का दामन फैलता तो है, मगर फिर भी छोटा ही पड़ जाता है। सुबह को घर से निकलने वाला शख़्स रात ही को वापस आ पाता है।
छुट्टी के दिन ही दिन में रहा अपने घर में मैं
बेटे ने मुझको बाप का दर्जा नहीं दिया
बच्चों को नौकरी मिल जाती तो बाप काहे को उनके पेट पालने के लिए अपने आराम के दिनों यानी बुढ़ापे में मेहनत और मशक्कत बादिले-नाख़्वास्ता करना-
मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़
मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते
समाज में एक और लानत ऐसी है कि जिस तरफ़ लोग बुरी नज़र से देखते तो हैं, मगर इस सिलसिले में कोई ठोस क़दम नहीं उठाते। शराबबंदी के सिलसिले में हुकूमत अपनी जगह सोचती है और मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से शराब की बुराइयों को अवाम के सामने रखती भी है, मगर इसको क्या किया जाए कि किसी ने इस जानिब कोई तवज्जोह ही न दी। मैं तो कहता हूं कुछ न करती, एक शेर हर दफ़्तर, हर चौराहे पर, हर गली के मोड़ पर जली हर्फ़ों में लिख कर चस्पां कर देती-
मयकदे में किसने कितनी पी ख़ुदा जाने मगर
मयकदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया
इस शेर को पढ़ने के बाद जाम उठाने से पहले मयनोश की उंगलियां एक बार थरथरातीं तो ज़रूर। तो साहब शायर तो अपना काम कर रहा है, मगर हुकूमत की आंखें नहीं खुलतीं। अरे जनाब सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। ये लिख देना सिगरेट की डिब्बियों पर अच्छा नहीं लगता। शराब बुरी है तो आप ये देखें कि शराब कौन कशीद कर रहा है। सिगरेट कहां तैयार की जा रही है। आप उन फैक्ट्रियों को ज़बरदस्ती बंद करवाएं। मगर नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे हुकूमत को अच्छी-ख़ासी आमदनी जो है और इक़्ितदार की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग पैसा कमाने ही तो आए हैं। वतन की ख़िदमत का जज़्बा किसमें है। शराब का ज़िक्र छिड़ ही गया है तो आइए आपको मौज़ू-ए-गुफ़्तगू से हटकर भी कुछ अच्छे शेर क्यों न सुना दूं, जो मुझे पसंद हैं-
तुम्हारी आंखों की तौहीन है ज़रा सोचो
तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है
मेरी एक शब भी न कट सकी
तेरे दैरो-काबा में नासेहा
यहां मय की कोई किरण नहीं
तेरी उम्र कैसे गुज़र गई
किसी के साथ कर लेना इबादत
हर इक के साथ मयख़्वारी न करना
और फिर आख़िर में ये नौबत भी आ जाती है कि जब शायर को कहना पड़ता है-
इक उम्र का चढ़ा हुआ नश्शा उतर गया
बेटे ने पी तो बाप का नश्शा उतर गया
आर्थिक या इक्तिसादी उलझनों से भी अवाम की ज़िंदगी बेपरवाह नहीं रह सकती। ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ों के दाम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई, कम तौल और मिलावट का धंधा इस क़दर परवान चढ़ा हुआ है कि ईमानदार आदमी का ज़िंदगी गुज़ारना दुश्वार ही नहीं, नामुमकिन-सा हो गया है। पहले उन पर निगाह डाल लें कि जिनके पास कई-कई कोठियां हैं, फ़ार्म हैं, मिलें हैं और फिर अपने मुल्क का मुक़द्दर हाथ में लेकर खिलवाड़ करते हुए हमारे नेता और आम इंसान के दरमियान ये फ़ासला क्या, ऐसा सोचने और फिर कह देने पर मजबूर नहीं कर देगा कि-
ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे
ये सब थे साथ मेरे भीख मांगने वाले
या
ये ही मेयार-दयानत है तो कल का ताजिर
बर्फ़ के बांट लिए धूप में बैठा होगा
मज़मून मुख़्तसर ही लिखना चाहा था, मगर ज़रा तवील हो गया। आप यक़ीन मानिए, ये मौज़ू ऐसा है कि जितना ग़ौर कीजिए, फैलता चला जाता है और कमाल ये है कि जी भी नहीं भरता, मगर दूसरों की बोरियत का भी तो ख़याल रखना चाहिए। वैसे भी मैं नस्र कहां लिख पाता हूं। बुनियादी तौर पर तो मैं शायर ही तो हूं। हां, शेर सुनिए कुछ ख़ूबसूरत बातों वाले, लबो-लह्जे वाले, ज़ुबान वाले और ख़याल वाले, मगर यहां मैं अपना कोई शेर न सुनाऊंगा, अपने दोस्तों के सुनाऊंगा, जो दूसरों के होते हुए भी हमेशा मुझे अपने से लगते हैं -
बदन तो ख़ुश है कि उस पर हैं रेशमी कपड़े
ज़मीर चीख़ रहा है कि बिक गया हूं मैं
हैं तो महफ़िल में मगर ऐसी जगह बैठे हैं
जामे-मय हादसा बन जाए तो हम तक पहुंचे
वो लोग जिनके पास चिराग़ों के ढेर हैं
वो लोग चाहते हैं बड़ी लंबी रात हो
ज़ह्र इस माहौल का इस दर्जा मुझमें भर गया
सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया
तुम अपने चेह्रे से नाराज़गी की बर्फ़ हटाओ
मैं मानती हूं कि सारी ख़ताएं मेरी हैं
क्या सितम करते हैं मिट्टी के खिलौने वाले
बैठे हैं राम को रक्खे हुए रावन के क़रीब
अपनी हद में रह के देना दान हो या दक्षिणा
वरना तुमको वक्त का रावण उठा ले जाएगा
वो मेरा हमसफ़र था, मगर मैं शिकस्ता पा
वो अपनी धुन में दोशे-हवा पर सवार था
कुछ इस जगह पे धूप की शिद्दत में है कमी
शायद यहां कोई शजरे-सायादार था
दुनिया-ए-तहज़ीबे-बशर के
तपते हुए सहराओं में
ऐसे भी कुछ पेड़ हैं जिनके
मीलों-मीलों साये हैं – "कृष्ण बिहारी नूर"
(यह पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको जखीरा.कॉम पर पढ़ने को मिलेगी)
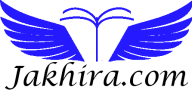




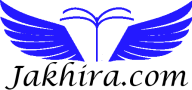





COMMENTS