धूप का टुकड़ा - योगेश गुप्त मैंने उससे कहा -- धीरे-धीरे चलो, तो वह अनायास ही मान गई | मुझे बहुत संकोच हुआ | वह किसी भी बात को इतनी जल्दी क्यों मान जाती

धूप का टुकड़ा - योगेश गुप्त
मैंने उससे कहा -- धीरे-धीरे चलो, तो वह अनायास ही मान गई | मुझे बहुत संकोच हुआ | वह किसी भी बात को इतनी जल्दी क्यों मान जाती है ? वह क्षण जब वह कहती है, "अच्छा," कितना लिजलिजा हो जाता है |
मैंने कहा था, "हर बात ऐसे मत मान जाया करो | लड़ते-भिड़ते चलने में ज्यादा आनंद है | समझी |"
उसने कहा, "अच्छा |"
उसका नाम सुधा है | खुबसूरत है | शिष्टाचार बरतना जानती है | चार दोस्त आते है तो बैठी हुई बुरी नहीं लगती | सलीके से उठकर चाय बनाने जाती है, करीने से प्याले मेज पर सजाती है | पर दोस्त उठकर चले जताए तो हमेशा झगडा होता है मै पूछता हूँ, "यह घर सराय है कि जब मर्जी जितने मर्जी लोगो के लिए चाय बने |"
"तुमने ही तो कहाँ था |"
"मैंने कहाँ! मुझे तो कहना पड़ता है | तुम कह देती कि दूध नहीं है या इस समय चाय बनाने की तुम्हारी तबियत नहीं है, या बाहर जाकर पी आओ |"
"मै क्यों कह देती ?"
--"मत कहो, घर लुटवा दो |"
उसने फिर करवट बदल ली, "अच्छा-अच्छा, अगली बार कह दूंगी |"
मै ठंडा हो जाता | मुझे लगता, जिस पेड़ पर मै चढ़ रहा हूँ वह धरती में धंसता जा रहा है | चढ़ने की थकान तो शरीर में है, ऊंचाई तक पहुँचने का गौरव मन में बिलकुल नहीं है |
मै अकस्मात सोचता हूँ, कमरे की खिडकियों पर पड़े परदे हटा दूँ | शीशे के गिलासों की जगह लकड़ी के गिलास लाकर रख दूँ | वह जग किसी को दे दूँ जिसमे कभी-कभी मै बियर पी लिया करता हूँ |
पर मै ऐसा क्यों सोचता हूँ ! सुधा को लेकर मै क्यों नाराज रहता हूँ ? ढूढने से भी कोई कारण नहीं मिलता | मैंने पसंद करके उसे शादी की है | उसके रूप के गुण पाए है, बालो को हाथ में लेकर बार-बार सुंघा है, चेहरे की मौलिक-से-मौलिक उपमा खोजने की कोशिश की है | फिर आज क्या हो गया ? पहली सब बातो पर हंसी क्यों आने लगी ? वह बुरी नहीं लगती, पर क्या वाकई अच्छी भी लगती है ? कोच पर पास बैठते ही मेरे शरीर में क्या चुभने लगता है ? उसके काले रंग में व्याप्त काले गुलाब की खुशबु कहाँ उड़ गई ? मै कौन हो गया हूँ ? वो कैसी हो गई है ?
एक दिन मैंने अपने पर दबाव डालकर कहाँ, "सुनो तुम्हे मालूम है, अब तुम मुझे पहले की तरह नहीं लगती ?"
उसने निहायत ठन्डे लहजे में कहाँ, "मालूम है !"
"कैसे ? "
"कैसे क्या ? मालूम है, बस ! ऐसा होता है |"
"क्या होता है ?"
"लोहा ठंडा होता है | तुम लोग लोहे के बने होते हो |"
मैंने कहा, "तुम लोगो में कोई परिवर्तन नहीं होता ?"
"होता है |"
"क्या ?"
"हम लोहे की ठंडक महसूस करती है |"
"फिर ? "
"फिर चुप हो जाती है और धीरे-धीरे सिर्फ हाँ मै हाँ मिलाने लगती है |"
उस दिन मै चुप रह गया था | महसूस हुआ जैसे सुधा ने खेल-खेल में दोनों हाथ पकड़ कर, घुमाकर मुझे अपनी जगह खड़ा कर दिया है और खुद मेरी जगह आकर ख़ड़ी हो गई -
शरारत से पूछ रही है, " अब बोलो ! बड़े होशियार बनते थे न !"
मै चुप हूँ |
मै हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ | इतनी बड़ी दुनिया, उसमे समाज-दर-समाज और उनमे अच्छे-बुरे लोग, नाते-रिश्ते ! उन सबकी भीड़ में चारो तरफ हार ही हार ! बड़े शहर, छोटे गाँव, पर हार-जीत का वही खेल और अंत में एक छोटा-सा घर ! एक पत्नी अच्छी-बुरी या जैसी भी और उससे भी हार ! चारो तरफ किवाड़ बहर से बंद और आपकी पत्नी कद में, अक्ल में, सामाजिक स्थिति में आपसे छोटी, आपकी मोहताज, आप पर हसती हुई - शांत भाव से, निरुद्विग्न, हसती हुई वह मुझे छोटा समझती है |
खाना खा लिया तो आदत के अनुसार बाद की चाय पीते हुए सुधा को अपने ठीक सामने बैठा पाकर कहा, "तुम मुझे अपने से छोटा समझती हो?"
उसने हसकर कहाँ, "छोटे तो तुम मुझसे हो ही|"
"उम्र में ?"
"पहले पैदा होने से कोई छोटा-बड़ा थोड़े ही हो जाता है |"
"तो फिर मै कैसे छोटा हूँ ?"
"तुम मुझसे प्यार करते हो ना ?"
"फिर ?"
"प्यार करने से आदमी छोटा हो जाता है |"
"तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती ?"
"करती थी |"
"कब ?"
"शादी से पहले | अब नहीं करती | अब सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ | तुम्हे पालती हूँ | तुम्हारी हर माँग पूरी करती हूँ | तुम्हे ध्यान तो होगा, तुम हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते थे | इसलिए मै तुम्हे अपने से छोटा समझती हूँ |"
"मैंने तुमसे क्या माँगा है ?"
वह हंस पड़ी, बोली "क्यों नहीं माँगा ?"
मै फिर बूंद होकर रहा गया | मुझे लगा , लोहे को किसी ने मात्र छू भर दिया है और वह अपना सारा व्यक्तित्व खो बैठा है |
अचानक मै घिघिया गया, "बहुत निर्मम हो, सुधा !"
"नहीं, उतनी निर्मम नहीं हूँ | हम लोगो में ममता थोड़ी बहुत किसी न किसी कोने में बची पड़ी रहती है |"
"अब क्या कहूँ ? कुछ भी नहीं रह गया | बरसो से इकट्ठे होते 'कुछ' के झरने के मुह पर अचानक चट्टान ख़ड़ी हो गई है |
मुझे अन्दर आभास हो रहा है कि मै सुधा को छोटा करने की बराबर भरसक चेष्टा करता रहा हूँ | सुधा यह बात जान गयी है और अब जान-बुझकर मुझे छोटा करने पर तुली है | इन लोगो का यह विचित्र नाटक है, विचित्र साहस है कि जिसके आधार पर जीवन बिताती है, जिसके न होने पर पलभर में वे अनाथ और निराधार तैरते पत्ते की तरह हो जाती है, उसे ही उम्र भर छोटा करने का प्रयास करती है | कितनी सीधी समझता था मै सुधा को ! हमेशा "हाँ में हाँ" मिलाने वाली | पर पलभर में कैसे काट गयी, कैसे बता गयी की "प्रेम करती नहीं हूँ, करती थी |"
हर दिन की तरह उस दिन भी शाम हुई | कमरे में खिड़की के सहारे आने वाला धूप का खिलौना आँख बचाकर भागने लगा | मुझे वह दृश्य देख अच्छा लगा | सुधा बीच-बीच में रसोई से कमरे में आकर कुछ न कुछ कर जाती थी | शायद कमरे की जगह मुझे टटोल रही थी | मै जाते हुए धुप के खिलौने के पास ही कुर्सी डाले बैठा था | मन में कुछ बहुत तीता, बहुत उत्तेजक तिरमिरा रहा था | मैंने आखिर धीरे से गाँठ खोली, "आज बड़ी व्यस्त लगती हो ?"
सुधा अपने उसी ठन्डे लहजे में बोली, "हाँ, खाली नहीं हूँ, बाहर घूम आओ |"
मैंने पूछा, "खाना कितनी देर में बन जायेगा ?"
"बन रहा है |"
संबंधो में पड़ी गाँठ सुलझाने से पहले नाखुन काट लेना बहुत जरुरी होता है | मन की गाँठ और सम्बन्ध की गाँठ में यही अंतर है |
पर मै क्या खोज रहा हूँ ? गाँठ या गाँठ खोलने का तरीका ? शायद मुझे गाँठ का ही परिचय नहीं है | मुझमे और सुधा में कोई गाँठ है ? नहीं तो, हम तो प्रेम में बंधे है ! फिर खोलना क्या चाहता हूँ, मुझे लगता है, कही कोई भारी गलती हो गयी है |
घूमकर, आकर मै फिर कोच में फैलकर बैठ गया | खाना खाया तो चुपचाप खा लिया | सुधा अब खाना रसोई में ही खाती है | वह खाकर आयी तो धीमे से पलंग पर बैठ गयी और पलंग पर पड़ा क्रोशिया-धागा उठा लिया | कमरे में अभी-अभी सफेदी हुई थी | बत्ती पहले से ज्यादा तेज लग रही थी | शाम को खेलता धूप का खिलौना अब बाहर खिड़की के निचे खेल रहा था | बाहर शायद तेज हवा चल रही थी | खिड़की के परदे के जरा-से उधडे होने से यह खिलौना अस्तित्व में आ गया था | मैंने खिड़की से झाककर देखा तो वह खेलता हुआ अच्छा लगा | पर तभी न जाने मेरे मन में क्या कोंधा कि मैंने पर्दा ठीक कर दिया और वह खिलौना फिस्स हो गया | बाहर गहरा अँधेरा छा गया |
सुधा मुस्कुरा दी |
"क्यों, हस क्यों रही हो ?"
"यों ही |"
"यो ही हसना तो बीमारी है |"
"हाँ, यह धीरे-धीरे पैदा होती है |"
"क्या मतलब ?"
"पर्दा क्यों ठीक कर दिया ?"
"यो ही |"
"परदे यों ही ठीक करना भी बीमारी है | बाहर अँधेरे में बना वह रौशनी का खिलौना तुमने यों ही मिटा दिया | ऐसे मिटाने का शौक और ...."
"और क्या ?"
"आदमी हिटलर बन जाता है |"
"तो मुझमे यह तत्व है ?"
"मै क्या जानू तुम जानो ! तुम तो हमेशा कहते हो की तुम अपने आपको अच्छी तरह जानते हो |"
"मै जैसे झुंझला उठा, "यह तुम मेरे साथ क्या किया करती हो ? मुझे अक्सर लगता है, तुम्हे मेरे दिमाग में पिन-सुई चुभने में मजा आता है |"
"बहुत मजा तो नहीं आता, पर हाँ, थोडा आलस्य तो टूटता ही है |"
"अच्छा ?"
"शायद !"
मै बौखला उठा, "मै किसी दिन तुम्हारी हत्या कर दूंगा | तुम जौंक की तरह मेरा खून चूस रही हो |"
"अच्छा !"
"अच्छा क्या ? यह हर समय "अच्छा-अच्छा" क्या होता है ! तुम क्या समझती हो, मै तुम्हारे बिना मार जाऊंगा ?"
"मेरी समझ इतनी दूर तक नहीं जाती |"
"ओह !"
"तुम चाहती क्या हो ?"
"तुमसे क्या चाहा जा सकता है ?"
"मै किसी योग्य नहीं हूँ ?"
"योग्यता की नहीं, सिद्धांत की बात है, तुम तो हमेशा कहते कि ..."
"क्या ?"
"ऐसा काम अच्छा होता है जिसका अच्छा-बुरा कोई फल न हो | काम और फल के बीच तूम रोक लगाते हो | तरह-तरह के तरीके अपनाते हो | निरर्थक श्रम, शायद तुम्हारा सिद्धांत बन चूका है, आनंद देता है | पहले-पहले हर फैशन सुख दे सकता है , पर ...." कहकर वह खिड़की की तरफ देखने लगी |
मै सन्न रह गया की वह क्या कह रही है ! मैंने देखा की उसकी आँखों में आंसू उबल आए है |
वह सुबक उठी तो उसने धीरे-धीरे मुझसे या शायद अपने आपसे कहाँ, "मै बिल्कुल अकेली हूँ |"
मै शायद बात समझ रहा था | ताजा सफेदी रौशनी तेज कर ही देती है | चुने में शायद रौशनी को भी तराशने की ताकत है |
मैंने धीरे-से खिड़की पर पड़े परदे को हल्का सा खोल दिया | बाहर धूप का खिलौना चपल भाव से खेलने लगा |
मैंने कहा था, "हर बात ऐसे मत मान जाया करो | लड़ते-भिड़ते चलने में ज्यादा आनंद है | समझी |"
उसने कहा, "अच्छा |"
उसका नाम सुधा है | खुबसूरत है | शिष्टाचार बरतना जानती है | चार दोस्त आते है तो बैठी हुई बुरी नहीं लगती | सलीके से उठकर चाय बनाने जाती है, करीने से प्याले मेज पर सजाती है | पर दोस्त उठकर चले जताए तो हमेशा झगडा होता है मै पूछता हूँ, "यह घर सराय है कि जब मर्जी जितने मर्जी लोगो के लिए चाय बने |"
"तुमने ही तो कहाँ था |"
मै हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ | इतनी बड़ी दुनिया, उसमे समाज-दर-समाज और उनमे अच्छे-बुरे लोग, नाते-रिश्ते ! उन सबकी भीड़ में चारो तरफ हार ही हार ! बड़े शहर, छोटे गाँव, पर हार-जीत का वही खेल और अंत में एक छोटा-सा घर ! एक पत्नी अच्छी-बुरी या जैसी भी और उससे भी हार ! चारो तरफ किवाड़ बहर से बंद और आपकी पत्नी कद में, अक्ल में, सामाजिक स्थिति में आपसे छोटी, आपकी मोहताज, आप पर हसती हुई - शांत भाव से, निरुद्विग्न, हसती हुई वह मुझे छोटा समझती है |
"मैंने कहाँ! मुझे तो कहना पड़ता है | तुम कह देती कि दूध नहीं है या इस समय चाय बनाने की तुम्हारी तबियत नहीं है, या बाहर जाकर पी आओ |"
"मै क्यों कह देती ?"
--"मत कहो, घर लुटवा दो |"
उसने फिर करवट बदल ली, "अच्छा-अच्छा, अगली बार कह दूंगी |"
मै ठंडा हो जाता | मुझे लगता, जिस पेड़ पर मै चढ़ रहा हूँ वह धरती में धंसता जा रहा है | चढ़ने की थकान तो शरीर में है, ऊंचाई तक पहुँचने का गौरव मन में बिलकुल नहीं है |
मै अकस्मात सोचता हूँ, कमरे की खिडकियों पर पड़े परदे हटा दूँ | शीशे के गिलासों की जगह लकड़ी के गिलास लाकर रख दूँ | वह जग किसी को दे दूँ जिसमे कभी-कभी मै बियर पी लिया करता हूँ |
पर मै ऐसा क्यों सोचता हूँ ! सुधा को लेकर मै क्यों नाराज रहता हूँ ? ढूढने से भी कोई कारण नहीं मिलता | मैंने पसंद करके उसे शादी की है | उसके रूप के गुण पाए है, बालो को हाथ में लेकर बार-बार सुंघा है, चेहरे की मौलिक-से-मौलिक उपमा खोजने की कोशिश की है | फिर आज क्या हो गया ? पहली सब बातो पर हंसी क्यों आने लगी ? वह बुरी नहीं लगती, पर क्या वाकई अच्छी भी लगती है ? कोच पर पास बैठते ही मेरे शरीर में क्या चुभने लगता है ? उसके काले रंग में व्याप्त काले गुलाब की खुशबु कहाँ उड़ गई ? मै कौन हो गया हूँ ? वो कैसी हो गई है ?
एक दिन मैंने अपने पर दबाव डालकर कहाँ, "सुनो तुम्हे मालूम है, अब तुम मुझे पहले की तरह नहीं लगती ?"
उसने निहायत ठन्डे लहजे में कहाँ, "मालूम है !"
"कैसे ? "
"कैसे क्या ? मालूम है, बस ! ऐसा होता है |"
"क्या होता है ?"
"लोहा ठंडा होता है | तुम लोग लोहे के बने होते हो |"
मैंने कहा, "तुम लोगो में कोई परिवर्तन नहीं होता ?"
"होता है |"
"क्या ?"
"हम लोहे की ठंडक महसूस करती है |"
"फिर ? "
"फिर चुप हो जाती है और धीरे-धीरे सिर्फ हाँ मै हाँ मिलाने लगती है |"
उस दिन मै चुप रह गया था | महसूस हुआ जैसे सुधा ने खेल-खेल में दोनों हाथ पकड़ कर, घुमाकर मुझे अपनी जगह खड़ा कर दिया है और खुद मेरी जगह आकर ख़ड़ी हो गई -
शरारत से पूछ रही है, " अब बोलो ! बड़े होशियार बनते थे न !"
मै चुप हूँ |
"शादी से पहले | अब नहीं करती | अब सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ | तुम्हे पालती हूँ | तुम्हारी हर माँग पूरी करती हूँ | तुम्हे ध्यान तो होगा, तुम हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते थे | इसलिए मै तुम्हे अपने से छोटा समझती हूँ |"वह जैसे कह रही है -- "तुम लोगो को अपने दिमाग पर बड़ा गर्व होता है | हमें दिमाग की जरुरत ही नहीं | तुम कभी हम पर गर्व करते हो तो कभी अपने यश पर, या मोटी तनख्वाह पर | हम तो चुपचाप तुम्हारी आँख-मिचौनी देखा करती है -- अपने आपसे | सच ही तुम लोग बच्चे होते हो, तमाशे में आये हुए बच्चे !"
मै हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ | इतनी बड़ी दुनिया, उसमे समाज-दर-समाज और उनमे अच्छे-बुरे लोग, नाते-रिश्ते ! उन सबकी भीड़ में चारो तरफ हार ही हार ! बड़े शहर, छोटे गाँव, पर हार-जीत का वही खेल और अंत में एक छोटा-सा घर ! एक पत्नी अच्छी-बुरी या जैसी भी और उससे भी हार ! चारो तरफ किवाड़ बहर से बंद और आपकी पत्नी कद में, अक्ल में, सामाजिक स्थिति में आपसे छोटी, आपकी मोहताज, आप पर हसती हुई - शांत भाव से, निरुद्विग्न, हसती हुई वह मुझे छोटा समझती है |
खाना खा लिया तो आदत के अनुसार बाद की चाय पीते हुए सुधा को अपने ठीक सामने बैठा पाकर कहा, "तुम मुझे अपने से छोटा समझती हो?"
उसने हसकर कहाँ, "छोटे तो तुम मुझसे हो ही|"
"उम्र में ?"
"पहले पैदा होने से कोई छोटा-बड़ा थोड़े ही हो जाता है |"
"तो फिर मै कैसे छोटा हूँ ?"
"तुम मुझसे प्यार करते हो ना ?"
"फिर ?"
"प्यार करने से आदमी छोटा हो जाता है |"
"तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती ?"
"करती थी |"
"कब ?"
"शादी से पहले | अब नहीं करती | अब सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ | तुम्हे पालती हूँ | तुम्हारी हर माँग पूरी करती हूँ | तुम्हे ध्यान तो होगा, तुम हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते थे | इसलिए मै तुम्हे अपने से छोटा समझती हूँ |"
"मैंने तुमसे क्या माँगा है ?"
वह हंस पड़ी, बोली "क्यों नहीं माँगा ?"
मै फिर बूंद होकर रहा गया | मुझे लगा , लोहे को किसी ने मात्र छू भर दिया है और वह अपना सारा व्यक्तित्व खो बैठा है |
अचानक मै घिघिया गया, "बहुत निर्मम हो, सुधा !"
"नहीं, उतनी निर्मम नहीं हूँ | हम लोगो में ममता थोड़ी बहुत किसी न किसी कोने में बची पड़ी रहती है |"
"अब क्या कहूँ ? कुछ भी नहीं रह गया | बरसो से इकट्ठे होते 'कुछ' के झरने के मुह पर अचानक चट्टान ख़ड़ी हो गई है |
मुझे अन्दर आभास हो रहा है कि मै सुधा को छोटा करने की बराबर भरसक चेष्टा करता रहा हूँ | सुधा यह बात जान गयी है और अब जान-बुझकर मुझे छोटा करने पर तुली है | इन लोगो का यह विचित्र नाटक है, विचित्र साहस है कि जिसके आधार पर जीवन बिताती है, जिसके न होने पर पलभर में वे अनाथ और निराधार तैरते पत्ते की तरह हो जाती है, उसे ही उम्र भर छोटा करने का प्रयास करती है | कितनी सीधी समझता था मै सुधा को ! हमेशा "हाँ में हाँ" मिलाने वाली | पर पलभर में कैसे काट गयी, कैसे बता गयी की "प्रेम करती नहीं हूँ, करती थी |"
हर दिन की तरह उस दिन भी शाम हुई | कमरे में खिड़की के सहारे आने वाला धूप का खिलौना आँख बचाकर भागने लगा | मुझे वह दृश्य देख अच्छा लगा | सुधा बीच-बीच में रसोई से कमरे में आकर कुछ न कुछ कर जाती थी | शायद कमरे की जगह मुझे टटोल रही थी | मै जाते हुए धुप के खिलौने के पास ही कुर्सी डाले बैठा था | मन में कुछ बहुत तीता, बहुत उत्तेजक तिरमिरा रहा था | मैंने आखिर धीरे से गाँठ खोली, "आज बड़ी व्यस्त लगती हो ?"
सुधा अपने उसी ठन्डे लहजे में बोली, "हाँ, खाली नहीं हूँ, बाहर घूम आओ |"
मैंने पूछा, "खाना कितनी देर में बन जायेगा ?"
"बन रहा है |"
संबंधो में पड़ी गाँठ सुलझाने से पहले नाखुन काट लेना बहुत जरुरी होता है | मन की गाँठ और सम्बन्ध की गाँठ में यही अंतर है |
पर मै क्या खोज रहा हूँ ? गाँठ या गाँठ खोलने का तरीका ? शायद मुझे गाँठ का ही परिचय नहीं है | मुझमे और सुधा में कोई गाँठ है ? नहीं तो, हम तो प्रेम में बंधे है ! फिर खोलना क्या चाहता हूँ, मुझे लगता है, कही कोई भारी गलती हो गयी है |
घूमकर, आकर मै फिर कोच में फैलकर बैठ गया | खाना खाया तो चुपचाप खा लिया | सुधा अब खाना रसोई में ही खाती है | वह खाकर आयी तो धीमे से पलंग पर बैठ गयी और पलंग पर पड़ा क्रोशिया-धागा उठा लिया | कमरे में अभी-अभी सफेदी हुई थी | बत्ती पहले से ज्यादा तेज लग रही थी | शाम को खेलता धूप का खिलौना अब बाहर खिड़की के निचे खेल रहा था | बाहर शायद तेज हवा चल रही थी | खिड़की के परदे के जरा-से उधडे होने से यह खिलौना अस्तित्व में आ गया था | मैंने खिड़की से झाककर देखा तो वह खेलता हुआ अच्छा लगा | पर तभी न जाने मेरे मन में क्या कोंधा कि मैंने पर्दा ठीक कर दिया और वह खिलौना फिस्स हो गया | बाहर गहरा अँधेरा छा गया |
सुधा मुस्कुरा दी |
"क्यों, हस क्यों रही हो ?"
"यों ही |"
"यो ही हसना तो बीमारी है |"
"हाँ, यह धीरे-धीरे पैदा होती है |"
"क्या मतलब ?"
"पर्दा क्यों ठीक कर दिया ?"
"यो ही |"
"परदे यों ही ठीक करना भी बीमारी है | बाहर अँधेरे में बना वह रौशनी का खिलौना तुमने यों ही मिटा दिया | ऐसे मिटाने का शौक और ...."
"और क्या ?"
"आदमी हिटलर बन जाता है |"
"तो मुझमे यह तत्व है ?"
"मै क्या जानू तुम जानो ! तुम तो हमेशा कहते हो की तुम अपने आपको अच्छी तरह जानते हो |"
"मै जैसे झुंझला उठा, "यह तुम मेरे साथ क्या किया करती हो ? मुझे अक्सर लगता है, तुम्हे मेरे दिमाग में पिन-सुई चुभने में मजा आता है |"
"बहुत मजा तो नहीं आता, पर हाँ, थोडा आलस्य तो टूटता ही है |"
"अच्छा ?"
"शायद !"
मै बौखला उठा, "मै किसी दिन तुम्हारी हत्या कर दूंगा | तुम जौंक की तरह मेरा खून चूस रही हो |"
"अच्छा !"
"अच्छा क्या ? यह हर समय "अच्छा-अच्छा" क्या होता है ! तुम क्या समझती हो, मै तुम्हारे बिना मार जाऊंगा ?"
"मेरी समझ इतनी दूर तक नहीं जाती |"
"ओह !"
"तुम चाहती क्या हो ?"
"तुमसे क्या चाहा जा सकता है ?"
"मै किसी योग्य नहीं हूँ ?"
"योग्यता की नहीं, सिद्धांत की बात है, तुम तो हमेशा कहते कि ..."
"क्या ?"
"ऐसा काम अच्छा होता है जिसका अच्छा-बुरा कोई फल न हो | काम और फल के बीच तूम रोक लगाते हो | तरह-तरह के तरीके अपनाते हो | निरर्थक श्रम, शायद तुम्हारा सिद्धांत बन चूका है, आनंद देता है | पहले-पहले हर फैशन सुख दे सकता है , पर ...." कहकर वह खिड़की की तरफ देखने लगी |
मै सन्न रह गया की वह क्या कह रही है ! मैंने देखा की उसकी आँखों में आंसू उबल आए है |
वह सुबक उठी तो उसने धीरे-धीरे मुझसे या शायद अपने आपसे कहाँ, "मै बिल्कुल अकेली हूँ |"
मै शायद बात समझ रहा था | ताजा सफेदी रौशनी तेज कर ही देती है | चुने में शायद रौशनी को भी तराशने की ताकत है |
मैंने धीरे-से खिड़की पर पड़े परदे को हल्का सा खोल दिया | बाहर धूप का खिलौना चपल भाव से खेलने लगा |
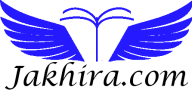




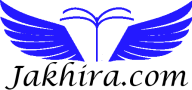





COMMENTS