शेख इब्राहीम ज़ौक परिचय खाकानी-ए-हिंद शेख इब्राहीम ज़ौक सन 1789 ई. में दिल्ली के एक गरीब सिपाही शेख मुह्ब्ब्द रमजान के घर पैदा हुए | शेख रमजान नवाब

शेख इब्राहीम ज़ौक परिचय
खाकानी-ए-हिंद शेख इब्राहीम "ज़ौक" सन १७८९ ई. में दिल्ली के एक गरीब सिपाही शेख मुह्ब्ब्द रमजान के घर पैदा हुए | शेख रमजान नवाब लुत्फ़अली खाँ के नौकर थे और काबुली दरवाजे के पास रहते थे | शेख इब्राहीम 'ज़ोंक' उनके इकलोटे बेटे थे | वे बचपन में मुहल्ले के एक अध्यापक हाफिज़ गुलाम रसूल के पास पढने जाया करते थे | हाफिज़ भी शायर थे और मदरसे में भी शेरो-शायरी की चर्चा होती रहती थी, इसीलिए इब्राहीम की तबियत भी इधर झुकी |
इनके एक सहपाठी मेरे काजिम हुसैन भी शायरी का शौक रखते थे | वे कभी-कभी जाकर हाफिज़ साहब से इस्लाह ( परामर्श) लेते थे | इब्राहीम की उनसे अच्छी दोस्ती थी |
एक बार की बात है | मियां इब्राहीम को इन्होने एक ग़ज़ल सुनाई जो इब्राहीम को बहुत पसंद आयी | पूछने पर काजिम हुसैन ने बताया की हम तो शाह नासिर के शार्गिद हो चुके है | शाह नासिर उस ज़माने के एक मशहूर शायर थे | यह ग़ज़ल उन्ही की संशोधित की हुई है | इस वजह से इब्राहीम साहब को भी शौक पैदा हुआ और उनके साथ जाकर शाह नासिर के शिष्य बन गये |
जब इब्राहीम वहा पहुचे, तो शाह नासिर ने इनके साथ वैसा सलूक नहीं किया, जैसा बुजुर्ग उस्ताद को करना चाहिए था | पर इससे ये निराश न हुए व शायरी करते रहे | उनके अन्दर काव्य-रचना की प्रतिभा प्रकृति-प्रदत्त थी, इसीलिए मुशायरो में इनकी काफी तारीफ होने लगी |
उन्ही दिनों शाह नासिर को अपनी उस्तादी के लिए खतरा पैदा होने लगा | उनके मन में विचार आया की कही शार्गिद उस्ताद से आगे न निकल जय, इसीलिए उन्होंने अपन ध्यान इब्राहीम की तरफ से हटा लिया | वह उनके साथ और भी बेरुखी बरतने लगे और कदम-कदम पर इन्हें निरुत्साहित भी करने लगे | वे उनकी ग़ज़लों में लापरवाही से इस्लाह देने लगे | और बात-बात पर इन्हें डाटा भी करते थे |
इसी हालत में एक दिन यह 'सौदा' की एक ग़ज़ल पर, ग़ज़ल लिखकर उस्ताद के पास ले गए | उन्होंने नाराज़ होकर ग़ज़ल फेक दी और कहा, " अब तू मिर्ज़ा रफ़ी सौदा से भी ऊँचा उड़ने लगा ?"
उस दिन वे निराश होकर जमा मस्जिद में जा बेठे | वहा एक बुजुर्ग शायर मेरे कल्लू 'हकीर' के प्रोत्साहन से ग़ज़ल मुशायरे में पढ़ी, तो वहा लोगो ने खूब वाहवाही की | उस दिन के बाद इब्राहीम ज़ौक ने शाह नासिर की शार्गिदी छोड़ दी |
जब ये उस्ताद से अलग हो गये तो उनको ख्याल आया की शहर में मिलने वाली ख्याति को आगे बढाकर लालकिले पहुचाया जाये | उन दिनों अकबर शाह द्वितीय बादशाह थे |
अकबर को कविता से कुछ लगाव नहीं था, लेकिन युवराज़ मिर्ज़ा अबू जफ़र स्वयं शायर थे और किले में अक्सर मुशायरे वगेरह हुआ करते थे | जिनमे उस समय के पुराने शायर आया करते थे, लेकिन मिया इब्राहीम एक गरीब सिपाही के बेटे थे, किसी रईस की जमानत के बिना किले में कैसे दाखिल हो सकते थे | काफी कोशिशो के बाद मेरे कासिम हुसैन की मध्यस्थता से किले के मुशायरे में शरीक होने का अवसर पाया | काजिम साहब खुद भी उस ज़माने के अच्छे शायरों में जाने जाते थे |
उन दिनों शाह नासिर युवराज़ के उस्ताद बने हुए थे, लेकिन एक दिन वह भी अंग्रेजो के मीर-मुंशी होकर पशिचम की और चले गये | ऐसे ही एक दिन इत्तफाक से युवराज़ जफ़र ने 'ज़ौक' को अणि ग़ज़ल दिखाई, जो अभी बिलकुल लड़के ही थे | उन्हें इनकी इस्लाह बहुत पसंद आयी | इस प्रकार उन्होंने इन्हें अपना उस्ताद बना लिया और तनख्वाह भी चार रुपया माहवार तय की गयी |
फिर यह तनख्वाह चार से सात रुपया हो गयी | वह चाहते तो इस तनख्वाह को ज्यादा भी करा सकते थे लेकिन उन्होंने जफ़र से कुछ नहीं कहा |
जोक के पिता ने उन्हें युवराज़ की इतनी कम तनख्वाह पर नौकरी करने से मना भी किया, लेकिन उन्हें युवराज़ का साथ इतना भा गया कि किसी बात का ख्याल ही नहीं किया | वह वहा जाकर नौकरी करते रहे |
इसके बाद १९ साल कि उम्र में आपने बादशाह अकबर के दरबार में एक कसीदा सुनाया | इस कसीदे का पहला शेर यह है-
जब कि सरतानो-अहद मेहर का ठहरा मसकन,
आबो-ए-लोला हुए नखो-नुमाए-गुलशन |
इस पर उन्हें खाकानी -ए-हिंद का ख़िताब मिला खाकानी फारसी भाषा का बहुत मशहूर कसीदा कहने वाला शायर था | १९ साल कि उम्र में यह ख़िताब पाना गर्व कि बात थी |
उनके हर शेर में हर अल्फाज़ किसी नगीने कि तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है | उनकी शायरी में तपिश हो या तल्खी, मासूमियत हो या प्यार लेकिन अंदाज ऐसा न होता था कि सुनने वाला मुग्ध हो जाए |
शेख मोहम्मद ज़ौक दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह जफ़र के समकालीन थे, इसीलिए उन्हें जफ़र का उस्ताद होने का भी गौरव प्राप्त था |
नए शायरों पर ज़ौक का ऐसा असर था कि वे उनकी शार्गिदी करना पसंद करते थे | उनके शागिर्दों कि संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे ज़ौक नाम से ही मशहूर हो गए |
अकबर शाह के निधन के बाद बहादुर शाह जफ़र जब बादशाह बने तो उनकी तनख्वाह सात रूपये से बढ़कर तीस रूपये महिना हो गई | ज़ौक को यह बेकदरी बहुत बुरी लगाती थी, मगर सवभाव में संतोष बहुत था | उन्होंने कभी बादशाह से इसकी शिकायत नहीं कि | इसी प्रकार ज़ौक के गरीबी के दिन कटते रहे |
अंत में ज़ौक कि तनख्वाह सौ रुपये कर दी गई | यह तनख्वाह भी उनकी योग्यता के सामने कुछ भी नहीं थी | तनख्वाह के अलावा ईद-बकरीद पर ईनाम भी मिला करते थे | अंतिम समय में उन्होंने बादशाह के बीमारी से अच्छे होने पर एक कसीदा पढ़ा | इस पर इन्हें खिलअत, खां बहादुरी का ख़िताब और चाँदी के हौदे के साथ एक हाथी मिला | फिर उन्होंने एक और कसीदा कहा, इस पर उन्हें एक गाव जागीर में मिला |
अंत में इस कमाल के उस्ताद ने 1271 हिजरी ( 1854 ई.) में सत्रह दिन बीमार रहकर परलोक गमन किया | मरने के तीन घंटे पहले उन्होंने यह शेर कहा था-
कहते है 'ज़ौक' आज जहा से गुजार गया,
क्या खूब आदमी था खुदा मग्फारत करे |
सच तो यह था कि ज़ौक अगर बहादुर शाह जफ़र कि उस्तादी से तौबा करके आज़ादी से शायरी करते तो और भी कई बेहतरीन ग़ज़ले व् शेर उर्दू अदब को दे जाते |
ज़ौक के अलावा लालकिले के मुशायरो में जो अन्य शायर शिरकत करने जाते थे, जिनको ज़ौक का बादशाह के साथ अधिक समय तक रहन अखरता था | विशेषकर ग़ालिब तो उन पर व्यंग्य भी कसते थे| पालकी में बेथ उनकी लाल किले में जाते देख ग़ालिब ने कहा
"बना है शह का मुसाहिब औ फिरे है इतराता"
ज़ौक ने इस बात कि शिकायत बादशाह से कि तो बादशाह ने वजह पूछी | ग़ालिब भी ज़ौक कि शायरी के प्रसंशक थे बस उन्हें ज़ौक कि बादशाह से निकटता पसंद नहीं थी उन्होंने जवाब दिया ," जनाब में तो ज़ौक साहब का मुरीद हू, इन्होने आधा शेर सुन गलत मतलब निकल दिया पूरा शेर है
" बना है शह का मुसाहिब औ फिरे है इतराता,
बगराना इस शहर में 'ग़ालिब' की आबरू क्या थी ?"
इनके एक सहपाठी मेरे काजिम हुसैन भी शायरी का शौक रखते थे | वे कभी-कभी जाकर हाफिज़ साहब से इस्लाह ( परामर्श) लेते थे | इब्राहीम की उनसे अच्छी दोस्ती थी |
एक बार की बात है | मियां इब्राहीम को इन्होने एक ग़ज़ल सुनाई जो इब्राहीम को बहुत पसंद आयी | पूछने पर काजिम हुसैन ने बताया की हम तो शाह नासिर के शार्गिद हो चुके है | शाह नासिर उस ज़माने के एक मशहूर शायर थे | यह ग़ज़ल उन्ही की संशोधित की हुई है | इस वजह से इब्राहीम साहब को भी शौक पैदा हुआ और उनके साथ जाकर शाह नासिर के शिष्य बन गये |
जब इब्राहीम वहा पहुचे, तो शाह नासिर ने इनके साथ वैसा सलूक नहीं किया, जैसा बुजुर्ग उस्ताद को करना चाहिए था | पर इससे ये निराश न हुए व शायरी करते रहे | उनके अन्दर काव्य-रचना की प्रतिभा प्रकृति-प्रदत्त थी, इसीलिए मुशायरो में इनकी काफी तारीफ होने लगी |
उन्ही दिनों शाह नासिर को अपनी उस्तादी के लिए खतरा पैदा होने लगा | उनके मन में विचार आया की कही शार्गिद उस्ताद से आगे न निकल जय, इसीलिए उन्होंने अपन ध्यान इब्राहीम की तरफ से हटा लिया | वह उनके साथ और भी बेरुखी बरतने लगे और कदम-कदम पर इन्हें निरुत्साहित भी करने लगे | वे उनकी ग़ज़लों में लापरवाही से इस्लाह देने लगे | और बात-बात पर इन्हें डाटा भी करते थे |
इसी हालत में एक दिन यह 'सौदा' की एक ग़ज़ल पर, ग़ज़ल लिखकर उस्ताद के पास ले गए | उन्होंने नाराज़ होकर ग़ज़ल फेक दी और कहा, " अब तू मिर्ज़ा रफ़ी सौदा से भी ऊँचा उड़ने लगा ?"
उस दिन वे निराश होकर जमा मस्जिद में जा बेठे | वहा एक बुजुर्ग शायर मेरे कल्लू 'हकीर' के प्रोत्साहन से ग़ज़ल मुशायरे में पढ़ी, तो वहा लोगो ने खूब वाहवाही की | उस दिन के बाद इब्राहीम ज़ौक ने शाह नासिर की शार्गिदी छोड़ दी |
जब ये उस्ताद से अलग हो गये तो उनको ख्याल आया की शहर में मिलने वाली ख्याति को आगे बढाकर लालकिले पहुचाया जाये | उन दिनों अकबर शाह द्वितीय बादशाह थे |
अकबर को कविता से कुछ लगाव नहीं था, लेकिन युवराज़ मिर्ज़ा अबू जफ़र स्वयं शायर थे और किले में अक्सर मुशायरे वगेरह हुआ करते थे | जिनमे उस समय के पुराने शायर आया करते थे, लेकिन मिया इब्राहीम एक गरीब सिपाही के बेटे थे, किसी रईस की जमानत के बिना किले में कैसे दाखिल हो सकते थे | काफी कोशिशो के बाद मेरे कासिम हुसैन की मध्यस्थता से किले के मुशायरे में शरीक होने का अवसर पाया | काजिम साहब खुद भी उस ज़माने के अच्छे शायरों में जाने जाते थे |
उन दिनों शाह नासिर युवराज़ के उस्ताद बने हुए थे, लेकिन एक दिन वह भी अंग्रेजो के मीर-मुंशी होकर पशिचम की और चले गये | ऐसे ही एक दिन इत्तफाक से युवराज़ जफ़र ने 'ज़ौक' को अणि ग़ज़ल दिखाई, जो अभी बिलकुल लड़के ही थे | उन्हें इनकी इस्लाह बहुत पसंद आयी | इस प्रकार उन्होंने इन्हें अपना उस्ताद बना लिया और तनख्वाह भी चार रुपया माहवार तय की गयी |
फिर यह तनख्वाह चार से सात रुपया हो गयी | वह चाहते तो इस तनख्वाह को ज्यादा भी करा सकते थे लेकिन उन्होंने जफ़र से कुछ नहीं कहा |
जोक के पिता ने उन्हें युवराज़ की इतनी कम तनख्वाह पर नौकरी करने से मना भी किया, लेकिन उन्हें युवराज़ का साथ इतना भा गया कि किसी बात का ख्याल ही नहीं किया | वह वहा जाकर नौकरी करते रहे |
इसके बाद १९ साल कि उम्र में आपने बादशाह अकबर के दरबार में एक कसीदा सुनाया | इस कसीदे का पहला शेर यह है-
जब कि सरतानो-अहद मेहर का ठहरा मसकन,
आबो-ए-लोला हुए नखो-नुमाए-गुलशन |
इस पर उन्हें खाकानी -ए-हिंद का ख़िताब मिला खाकानी फारसी भाषा का बहुत मशहूर कसीदा कहने वाला शायर था | १९ साल कि उम्र में यह ख़िताब पाना गर्व कि बात थी |
उनके हर शेर में हर अल्फाज़ किसी नगीने कि तरह पिरोया हुआ प्रतीत होता है | उनकी शायरी में तपिश हो या तल्खी, मासूमियत हो या प्यार लेकिन अंदाज ऐसा न होता था कि सुनने वाला मुग्ध हो जाए |
शेख मोहम्मद ज़ौक दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह जफ़र के समकालीन थे, इसीलिए उन्हें जफ़र का उस्ताद होने का भी गौरव प्राप्त था |
नए शायरों पर ज़ौक का ऐसा असर था कि वे उनकी शार्गिदी करना पसंद करते थे | उनके शागिर्दों कि संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे ज़ौक नाम से ही मशहूर हो गए |
अकबर शाह के निधन के बाद बहादुर शाह जफ़र जब बादशाह बने तो उनकी तनख्वाह सात रूपये से बढ़कर तीस रूपये महिना हो गई | ज़ौक को यह बेकदरी बहुत बुरी लगाती थी, मगर सवभाव में संतोष बहुत था | उन्होंने कभी बादशाह से इसकी शिकायत नहीं कि | इसी प्रकार ज़ौक के गरीबी के दिन कटते रहे |
अंत में ज़ौक कि तनख्वाह सौ रुपये कर दी गई | यह तनख्वाह भी उनकी योग्यता के सामने कुछ भी नहीं थी | तनख्वाह के अलावा ईद-बकरीद पर ईनाम भी मिला करते थे | अंतिम समय में उन्होंने बादशाह के बीमारी से अच्छे होने पर एक कसीदा पढ़ा | इस पर इन्हें खिलअत, खां बहादुरी का ख़िताब और चाँदी के हौदे के साथ एक हाथी मिला | फिर उन्होंने एक और कसीदा कहा, इस पर उन्हें एक गाव जागीर में मिला |
अंत में इस कमाल के उस्ताद ने 1271 हिजरी ( 1854 ई.) में सत्रह दिन बीमार रहकर परलोक गमन किया | मरने के तीन घंटे पहले उन्होंने यह शेर कहा था-
कहते है 'ज़ौक' आज जहा से गुजार गया,
क्या खूब आदमी था खुदा मग्फारत करे |
सच तो यह था कि ज़ौक अगर बहादुर शाह जफ़र कि उस्तादी से तौबा करके आज़ादी से शायरी करते तो और भी कई बेहतरीन ग़ज़ले व् शेर उर्दू अदब को दे जाते |
ज़ौक के अलावा लालकिले के मुशायरो में जो अन्य शायर शिरकत करने जाते थे, जिनको ज़ौक का बादशाह के साथ अधिक समय तक रहन अखरता था | विशेषकर ग़ालिब तो उन पर व्यंग्य भी कसते थे| पालकी में बेथ उनकी लाल किले में जाते देख ग़ालिब ने कहा
"बना है शह का मुसाहिब औ फिरे है इतराता"
ज़ौक ने इस बात कि शिकायत बादशाह से कि तो बादशाह ने वजह पूछी | ग़ालिब भी ज़ौक कि शायरी के प्रसंशक थे बस उन्हें ज़ौक कि बादशाह से निकटता पसंद नहीं थी उन्होंने जवाब दिया ," जनाब में तो ज़ौक साहब का मुरीद हू, इन्होने आधा शेर सुन गलत मतलब निकल दिया पूरा शेर है
" बना है शह का मुसाहिब औ फिरे है इतराता,
बगराना इस शहर में 'ग़ालिब' की आबरू क्या थी ?"
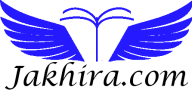




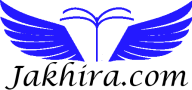





कहते है 'ज़ौक' आज जहा से गुजार गया,
ReplyDeleteक्या खूब आदमी था खुदा मग्फारत करे |
अच्छी जानकारी मिली।
मनोज जी धन्यवाद |
ReplyDelete